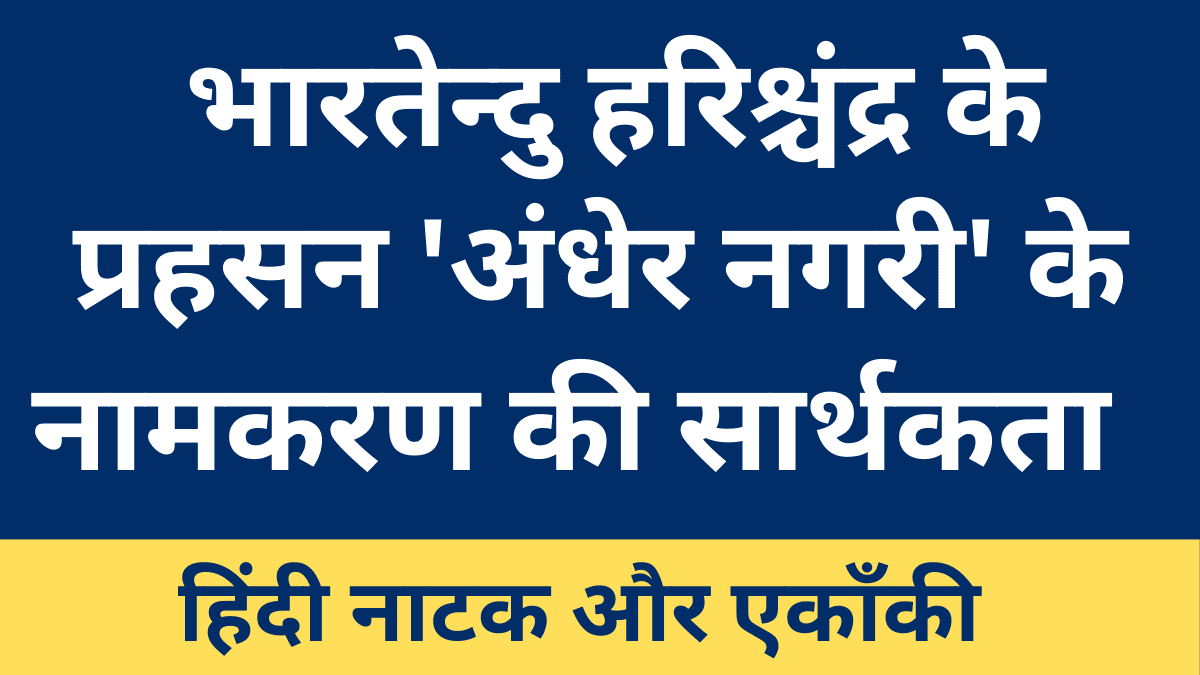‘अंधेर नगरी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का अत्यंत प्रसिद्ध प्रहसन है, जो 1881 ई. में प्रकाशित हुआ था । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने प्रहसन ‘अंधेर नगरी’ को परम्परा से चली आ रही लोकोक्ति ‘अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा’ पर आधारित किया है जिसमें बिहार के किसी मूर्ख और अत्याचारी शासक को आधार बनाकर उसके कुकर्मों को प्रकट किया है। तो आइये अब हम andher nagari ke namkaran ki sarthakta पर विचार करें ।
एक सामान्य सी लोकोक्ति के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के दोषों, शोषण, स्वार्थपरता आदि को एक साथ प्रकट करके अपने कौशल को प्रकट कर दिया है।
सामान्य रूप से किसी वस्तु को पहचानने के लिए उसे कोई-न-कोई नाम अवश्य दिया जाता है, जिससे उसकी विशिष्टता बनी रहे। साहित्यिक क्षेत्र में भी रचना का नाम, उसकी अलग पहचान बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है।
नाटक के क्षेत्र में नामकरण का बहुत महत्त्व है। फिर भी नामकरण से सम्बन्धित विस्तृत शास्त्रीय विवेचन नहीं प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य में नाटकों का नामकरण सामान्यतः निम्नलिखित आधारों पर प्राप्त होता है-
नायक के नाम पर
जो नाटक नायक प्रधान होते हैं, उनका नामकरण नायक के नाम पर किया जाता है। जैसे-अशोक, चन्द्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, नाना फड़नवीस आदि।
नायिका के नाम पर
जो नाटक नायिका प्रधान होते हैं, उनका नामकरण नायिका के नाम पर किया जाता है। जैसे ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, श्री चन्द्रावली, नीलदेवी, पद्मावती आदि।
मूल भाव पर
जिन नाटकों का नामकरण उनके उद्देश्य अथवा मूल भाव पर आधारित होता है वे इस श्रेणी में आते हैं। जैसे-धर्मालाप, तन-मन-धन गोसाई जी के अर्पण, कल्याणी परिणय, चक्रव्यहू, गोरक्षा, गोसंकट आदि।
घटना के आधार पर
नाटक में घटित किसी घटना के आधार पर किया गया नामकरण इस श्रेणी में आता है। जैसे सज्जन, जनमेजय का नाग यज्ञ, सिन्दूर की होली, राखी की लाज, अभिमन्यु वध, आहुत्ति, रक्षा बन्धन अदि ।
स्थान के नाम पर
किसी स्थान के नाम पर जिन नाटकों का नामकरण किया जाता है, वे इस श्रेणी में आता है। जैसे पाकिस्तान, वितस्ता की लहरें, कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, चित्रकूट आदि।
प्रतीकात्मकता के आधार पर
इस प्रकार के नामकरण नाटक में व्यक्त भावों, लक्षणों, प्रतीकों आदि के आधार पर किए जाते हैं। जैसे- भारत दुर्दशा, कामना, अंधेर नगरी, धूप-छांव, राक्षस का मन्दिर, लहरों का राजहंस, अंधा युग, करुणालय आदि।
नाटक के नामकरण के लिए लेखक चाहे कोई भी पद्धत्ति क्यों न अपनायें, अपनी रचना का नामकरण करने से पूर्व उसे उस नाटक के मूल-कथ्य, पात्र, उद्देश्य मूल-भाव आदि का विशेष ध्यान रखना रखना पड़ता है।
नामकरण सरल, मौलिक, संक्षिप्त एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। आकर्षक एवं उपयुक्त नामकरण वाली रचना पाठक एवं आलोचक को स्वयं ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।
यदि ‘अंधेर नगरी’ के नामरकण की सार्थकता को परखा जाए तो इसे विभिन्न आधारों पर स्थापित करना होगा। andher nagari ke namkaran ki sarthakta को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है :
ऐतिहासिक आधार
हमारा देश विभिन्न जातियों, धर्मों, सम्प्रदायों, भाषाओं आदि को सदा प्रश्रय देता (सहारा देना, आश्रय स्थान देना) रहा है और यही इसे तोड़ने और खण्डित करने का आधार बना रहा है।
यह एक नहीं अपितु, अनेक बार विदेशियों का गुलाम बना है। शक, हूण, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ आदि ने हमारा शोषण किया, हमें कुचला लेकिन हर बार हमारी गुलामी का मूल कारण आपसी भेदभाव, साम्प्रदायिक, मतभेद और धर्म के नाम पर वैर-भाव ही रहे।
हमारा इतिहास इस तथ्य का सदा साक्षी है कि हम अपनों से सदा हारे हैं तथा उनके कारण दूसरों के द्वारा हराये गए है। हमारी आपसी फूट हमारे घर को तोड़ती रही है। भारतेन्दु ने इस तथ्य को गम्भीरता से लिया था तभी तो उन्होंने कुंजड़िन के मुंह से कहलवाया था-
ले हिन्दुस्तान का मेवा फूट और बैर।
मानव का स्वभाव है कि कोई कभी स्वयं को धोखा नहीं देता लेकिन हम स्वयं को धोखा दे कर इसे ‘अंधेर नगरी’ बनाने का प्रयत्न करते रहे हैं।
सामाजिक आधार
लेखक ने नाटक के आधार रूप में जिस समाज को ग्रहण किया है वह अंग्रेजी शासन काल का समाज है जो भ्रष्ट शासकों के कारण से भ्रष्ट हो गया था।
सारे समाज में अराजकता थी, अन्यायपूर्ण और विकृत व्यवस्था थी। सर्वत्र लालच, शोषण और स्वार्थपरता पनप रही थी-
(क) चना हाकिम सब जो खाते।
सब पर दूना टिकस लगाते ।
(ख) चूरन सभी महाजन खाते।
जिससे जमा हजम कर जाते ।।
(ग) चूरन पुलिस वाले खाते।
सब कानून हजम कर जाते ।।
(घ) वेश्या जोरु एक समाना।
बकरी गऊ एक करि जाना ।।
(ङ) भीतर होइ मलिन की कारो।
चहिए बाहर रँग चटकारो ।।
तत्कालीन समाज बाहर से चाहे जैसा भी दिखता हो पर भीतर से मर्यादाहीन हो गया था। यह अन्धी व्यवस्था, अन्धे कानून और विवेकशून्य व्यवस्था का प्रतीक बनकर रह गया था।
अंग्रेज सरकार इसकी अवनति का कारण बनती जा रही थी। लेखक ने प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर यह बताना चाहा है कि अंग्रेजी कानून, न्याय व्यवस्था और शासनतन्त्र दूषित था। उस समाज में पण्डित और मूर्ख में कोई भेद नहीं था, शोषक और शोषित एक समान थे, अपराधी और निरपराधी में कोई अंतर नहीं था।
धार्मिक आधार
अंग्रेजी शासनकाल में हमारे देश में धार्मिक भेद-भाव को बढ़ावा मिला था। धर्म के नाम पर वैर-भाव बढ़ गया था। यह बाज़ार में बिकने वाली एक वस्तु बनकर रह गई थी। धर्म और जातियां विखण्डित होने लगी थी।
बाज़ार में हलवाई इसी बात की पुष्टि करता है- ऐसी जात हलवाई जिसके छत्तीस कौम हैं भाई !
उस समय धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ने लगा था। पण्डे-पुजारी स्त्रियों का शील-हरण का षड्यन्त्र रचने लगे थे। जातवाला ब्राह्मण तो स्पष्ट रूप से धर्म के क्षेत्र में अंधेर नगरी के नामकरण का आधार स्पष्ट कर देता है-
जात ले जात, टके सेर जात। एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिन्दू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें।
लेखक ने प्रकट करना चाहा है कि तत्कालीन धार्मिक परिवेश ‘अंधेर नगरी’ के अंधी विवेकहीन मान्यताओं का था। जिसमें परम्परागत उच्च धार्मिक मान्यताओं का पूर्णरूप से हनन हो रहा था।
वेद, धर्म, कुल, मर्यादा आदि सब टके सेर बिकने लगे। धर्म में ठेकेदार, प्रजा को दिशा दिखाने वाले सन्त-महात्मा, समाज के व्यवस्थापक आदि सब पेट की चिन्ता में व्यस्त रहने वाले थे। धर्म तो मात्र एक व्यापार बनकर रह गया था।
गोवर्धनदास का कथन इसी बात की पुष्टि करता है, “माना की देश बहुत बुरा है। पर अपना क्या? अपने किसी राज-काज में थोड़े हैं कि कुछ डर है, रोज मिठाई चाभना, मजे में आनन्द से राम भजन करना।” उस समय सन्त महात्मा आत्मकेन्द्रित थे और स्वार्थ में लिप्त थे।
अविवेकी शासक
भारतेन्दु ने अपने नाटक का आधार बिहार के किसी शासक को बनाया है जो किसी भी दृष्टि से शासक बनने योग्य नहीं था।
‘जैसा राजा वैसी प्रजा’ के आधार पर प्रजा को भी उसी के अनुरूप बदल जाना था। ‘चौपट्ट राजा’, साभिप्राय शब्द है। इस का सम्बन्ध ऐसे राजा से है जिसने अपने अविवेक, दुराचरण और दुर्बुद्धिपूर्ण नीतियों से सारे देश को चौपट कर दिया हो। जिसके कारण देश का सर्वनाश हो रहा हो जनता दुःखी हो।
इस नाटक में चौपट्ट राजा अविवेकी है, मूर्ख है, नशेबाज है। वह हर समय नशे में डूबा रहता है और साधारण सी बात भी उसकी बुद्धि में ठीक प्रकार से नहीं घुसती।
वह गाली-गलौच करता है तथा अपना दोष दूसरों के मत्थे मढ़ देना चाहता है। वह न्याय-अन्याय में अन्तर नहीं जानता। वह चरित्र से गिरा हुआ है और एक पत्नीव्रत नहीं है।
उसके इस कथन से “मंत्री बेर-बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है।” स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यभिचारी है तथा अन्य नारियों से उसके सम्बन्ध हैं।
वह अन्धविश्वासी है। वह अहंकारी तथा निरंकुश है तभी तो वैकुण्ठ जाने के अवसर पर वह कहता है, “चुप रहो, सब लोग। राजा के आछत और कौन बैकुण्ठ जा सकता है।”
लेखक ने चौपट्ट राजा के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को माना है जिस कारण सारा देश अराजकता का शिकार हो गया है।
सर्वत्र मूल्यहीनता की स्थिति है तथा गुण-ग्राह्यता समाप्त हो गई है। सब ओर अन्धाधुन्ध मची है, पूर्ण निरकुंशता का राज्य है। विदेश से इस देश का राजकाज अंग्रेज चला रहे है। यहाँ का धन लूटकर वे अपने देश ले जा रहे हैं-
(क) भीतर स्वाहा बाहर सादे ।
राज करहिं अमले अरु प्यादे ।।
(ख) अन्धाधुन्ध मच्यौ सब देसा।
मानहुँ राजा रहत विदेसा ।।
भ्रष्टराज में भ्रष्टाचारी पनप रहे है जिनके सामने भले लोगों की एक नहीं चलती। अंग्रेजी राज में देश की आर्थिक स्थिति कुछ खराब है जिस कारण यहाँ रहने वाला कोई व्यक्ति मोटा ही नहीं होता।
निष्कर्ष
नाटक में प्रस्तुत विभिन्न प्रसंगों और संवादों के आधार पर यही प्रमाणित होता है कि जब देश का राजा ही धूर्त, कपटी ओर अविवेकी होगा तो देश की जनता या प्रजा का पतन होना अनिवार्य है।
भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर इस नाटक का नामकरण ‘अंधेर नगरी’ किया है, जो पूर्ण रूप से सार्थक है। नाटक का उद्देश्य, कथ्य और प्रतिपाद्य इस के द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं इसलिए यह नामकरण पूर्ण रूप से सार्थक है। इस प्रकार andher nagari ke namkaran ki sarthakta पूरी तरह से स्पष्ट है ।

नमस्कार ! मेरा नाम भूपेन्द्र पाण्डेय है । मेरी यह वेबसाइट शिक्षा जगत के लिए समर्पित है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और अनुवाद विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य है । मैं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ।
मेरे लेक्चर्स हिंदी के छात्रों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं ।
मेरी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है : बीएससी, एमए (अंग्रेजी) , एमए (हिंदी) , एमफिल (हिंदी), बीएड, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन (गोल्ड मेडल), यूजीसी नेट (हिंदी), सेट (हिंदी)
मेरे यूट्यूब चैनल्स के नाम : Bhoopendra Pandey Hindi Channel, Hindi Channel UPSC