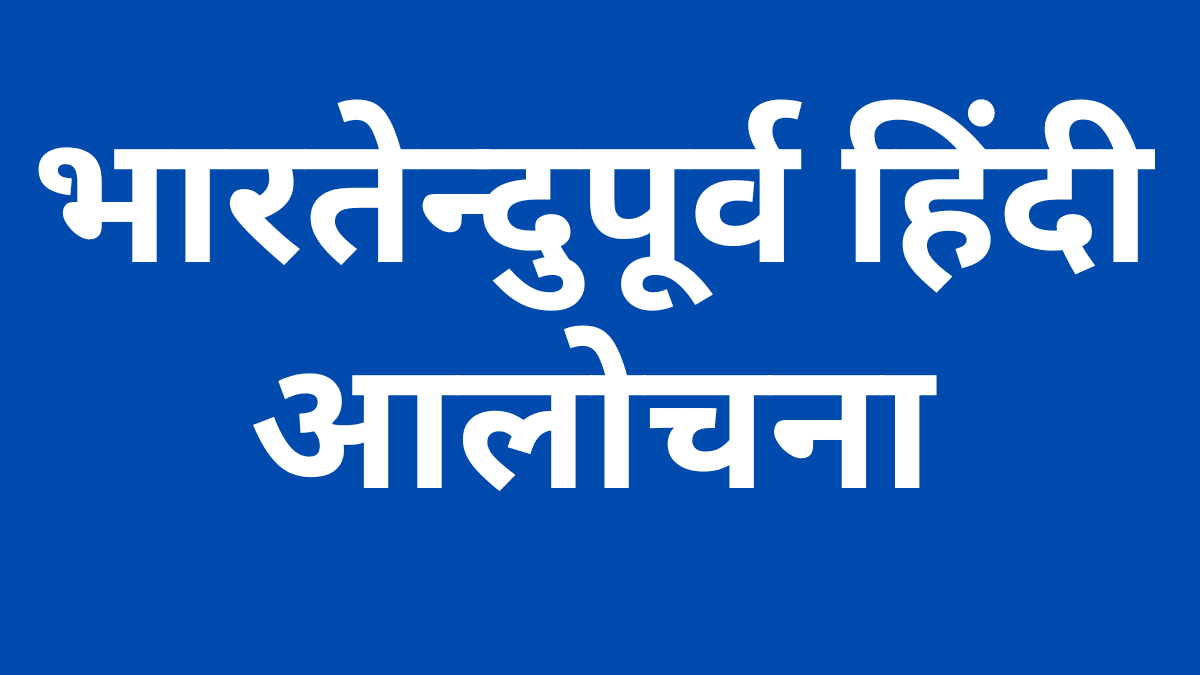भारतेन्दु से पूर्व भक्ति और रीति युग में आलोचना के क्षेत्र में प्रयास हुए हैं। भक्ति काल में भक्ति का प्रभाव इतना प्रबल है कि वहाँ अलग से काव्य-सिद्धांतों की चर्चा प्रायः नहीं हुई है। भक्त कवियों के लिए काव्य रचना ईश्वर भक्ति का साधन है इसलिए जहाँ ईश्वर है वहाँ उत्तम काव्य भी है।
कबीर, सूर तुलसी, मीरा भक्तिकाल के ये सभी भक्त कवि इसी आदर्श को मानते हैं। यद्यपि तुलसीदास ने “सुरसरि सम सब कह हित होई” तथा “गिरा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न” कह कर काव्य के प्रति अपनी सजगता भी प्रकट की है।
वैसे इसकाल में भक्तों के जीवन, विचार, भक्ति से परिचित कराने वाले ग्रंथ लिखे जाने लगे थे जिन्हें ‘वार्ता साहित्य’ के नाम से जाना जाता है। भक्त कवियों की कविता के संबंध में भी कहीं-कहीं विचार हुआ है। काव्य के वर्ण्य विषय और शैली बंधी विशेषताओं के अतिरिक्त काव्य के जन-साधारण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख हुआ है किंतु इनमें प्रशंसात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया गया है।
भक्तमाल में सूर के संबंध में इसी तरह विचार किया गया है।
उक्ति चोज अनुप्रास बरन-अस्थिति अति भारी।
बच्चन प्रीति निर्बाह अर्थ अद्भुत तुक धारी ॥
प्रतिबिम्बित दिवि दिष्टि हृदय हरि लीला भासी।
जनम करण गुण रूप रसना कर कासी ॥
(भक्तमाल)
इसी प्रकार बल्लभाचार्य ने सूर की भक्ति और कविता पर प्रसंगवश जो कुछ भी कहा है, उसमें आलोचना के तत्व निहित हैं। रीतिकाल में मौलिक विचारों की प्रवृत्ति तो है किंतु गूढ़ चिंतन और विषय के शास्त्रीय एवं यथार्थ ज्ञान का अभाव है। इसका कारण यही हो सकता है कि उस काल में गद्य रचना की पुष्ट परंपरा नहीं थी।
रीतिकाल का कवि पहले काव्य के अंगों का लक्षण देता था और बाद में स्वरचित कविताओं को उदाहरण स्वरूप रख देता था। कुछ आचार्यों ने अपने काल के अन्य कवियों की कविताओं का भी उदाहरणों में उपयोग किया है। इस काल में रीति-ग्रंथ बहुत लिखे गए।
आचार्यों ने प्रायः काव्य के सभी अंगों पर स्थूल रूप से विचार प्रकट किए। इस युग में संस्कृत समीक्षा शास्त्र की कई शैलियों का अनुकरण किया गया। अनेक कवियों का काव्य शास्त्रीय विवेचन तो आचार्यत्व की कोटि तक पहुँच गया। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं – आचार्य केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, पद्माकर, भिखारीदास, देव, घनानंद, मतिराम, बिहारी आदि।
इनमें आलोचना की दो विशिष्ट धाराओं को देखा जा सकता है –
• अलंकारवादी
• रसवादी
अलंकारवादी धारा के प्रवर्त्तक केशवदास है तो रसवादी धारा के प्रवर्तक देव, मतिराम और बिहारी ।
हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम आचार्य केशवदास माने जाते हैं। संस्कृत के अच्छे विद्वान होने के कारण उन्होंने अलंकार शास्त्र का निरूपण हिंदी में सफलता पूर्वक किया। उन्होंने ‘रसिकप्रिया’ और ‘कवि प्रिया’ में अलंकार शास्त्र के प्रायः सभी विषयों का प्रतिपादन किया।
‘रसिक प्रिया’ का विषय रस है, इसमें श्रृंगार को ही प्रधानता दी गई है। केशवदास रचित ‘रामचंद्रिका’ छंदों, अलंकारों और अन्य काव्य-अंगों के उदाहरणों का संग्रह है, साथ ही इसके माध्यम से कवि ने प्रबंध काव्य के शास्त्रीय रूप का भी एक उदाहरण हिंदी साहित्य के सामने रखा है।
चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति, दास और प्रतापसिंह जैसे आचार्यों ने संस्कृत समीक्षा के अनुकरण पर ग्रंथों की रचना की। ये
सभी आचार्य अलंकारवादी धारा के प्रतिनिधि हैं। इस धारा में चिंतामणि रचित ‘कवि-कुल-कल्पतरु’ और ‘काव्य विवेक’, सेनापति का ‘काव्य कल्पद्रुम’, श्रीपति का ‘काव्य सरोज’, प्रतापसिंह कृत ‘काव्यविलास’ तथा देव रचित ‘शब्द रसायन’ उल्लेखनीय हैं।
कवि देव मुख्यतः रसवादी धारा के हैं लेकिन अलंकार शैली में भी उन्होंने रचना की है। रसवादी धारा के आचार्यों ने श्रृंगार रस और नायिका भेद को प्रधानता दी। इस शैली की विशेष उल्लेखनीय पुस्तकें हैं केशवदास की ‘रसिक प्रिया’, देव कृत भावविलास’, ‘रस विलास’, भिखारीदास का ‘काव्य निर्णय’, पद्माकर रचित ‘जगद्विनोद’, मतिराम की ‘रसराज’ तथा बिहारी की ‘बिहारी सतसई’ ।
रीतिकाल में पद्यबद्ध टीकाएँ भी लिखी गई हैं। इनकी विशेषता आलोच्य वस्तु के अर्थ को अधिक स्पष्ट करना है किंतु काव्य में निहित सौंदर्य का निर्देश नहीं हुआ है। परन्तु , राजस्थान की कृति ‘क्रिसन रुक्मिणी री बेलि’ की कई टीकाएँ लिखी गई हैं। इनमें अलंकार निर्देश और काव्य सौष्ठव का विश्लेषण हुआ है।
कुछ टीकाएं राजस्थानी गद्य में भी लिखी गई। रीतिकाल के कुछ आचार्यों ने ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग भी किया लेकिन गद्य का सम्यक विकास उस समय तक न होने के कारण अधिक सफलता नहीं मिल सकी।
वंशीधर और दलपति ने केशव, गंग, बिहारी, मतिराम आदि के छंदों के उदाहरण दिए और अलंकार युक्त अंशों का निर्देश कर दिया। उन्होंने भी गद्य का प्रयोग किया।
रीतिकालीन समीक्षा के आदर्श के अनुकूल शास्त्रीय समीक्षा का प्रौढ़ उदाहरण है सरदार कवि कृत ‘मानस रहस्य’ । यह ग्रंथ सूत्र-शैली में लिखा गया है तथा सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें रामचरित मानस की व्याख्या की गई है। कहीं-कहीं गद्य में भी विवेचन किया है। एक उदाहरण
प्रस्तुत है –
“निज कर भूसन राम
बनाए सीताहि पहिराये प्रभुसादर”
निष्कर्ष
आलोचना का आधार युगीन साहित्यिक अपेक्षाएँ होती हैं। भक्तिकालीन और रीतिकालीन आलोचना के मानदंड आधुनिक साहित्य की आलोचना के लिए पर्याप्त न थे। अतः आलोचना को विकसित करना जरूरी हो गया।

नमस्कार ! मेरा नाम भूपेन्द्र पाण्डेय है । मेरी यह वेबसाइट शिक्षा जगत के लिए समर्पित है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और अनुवाद विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य है । मैं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ।
मेरे लेक्चर्स हिंदी के छात्रों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं ।
मेरी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है : बीएससी, एमए (अंग्रेजी) , एमए (हिंदी) , एमफिल (हिंदी), बीएड, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन (गोल्ड मेडल), यूजीसी नेट (हिंदी), सेट (हिंदी)
मेरे यूट्यूब चैनल्स के नाम : Bhoopendra Pandey Hindi Channel, Hindi Channel UPSC