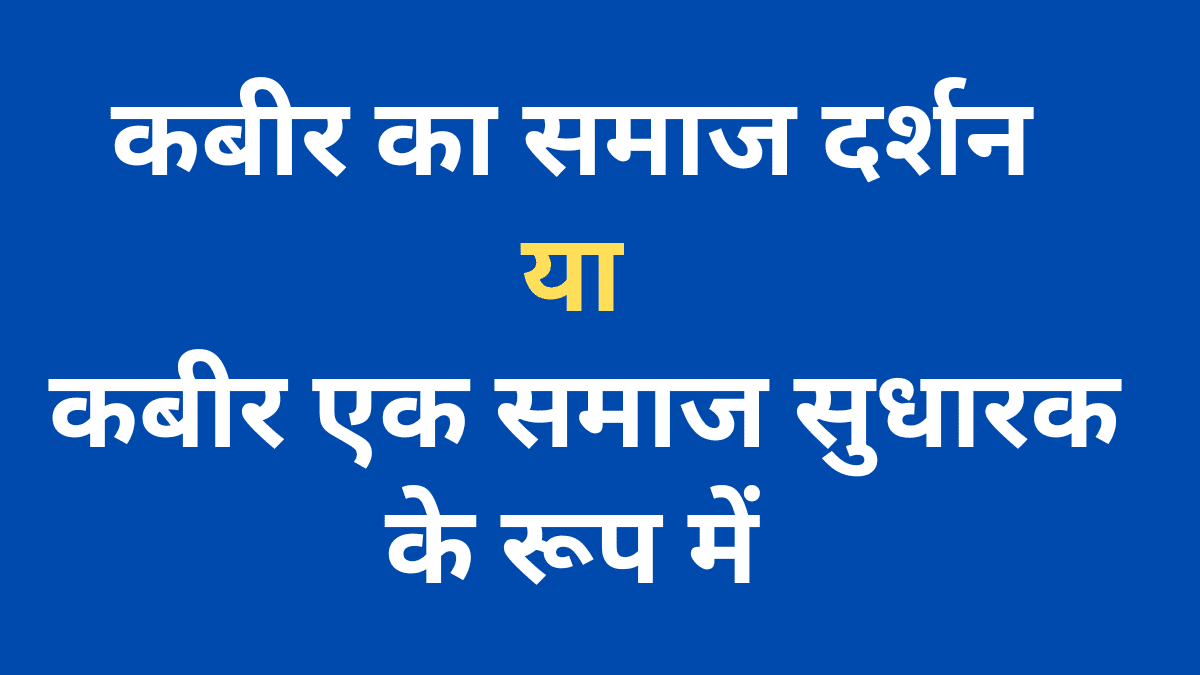आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल (पूर्व-मध्यकाल) का समय संवत् 1375 से 1700 (अर्थात् सन् 1318 ई. से 1643 ई.) तक है । उन्होंने भक्तिकाल का विभाजन निम्नानुसार किया है, जो आज सर्वमान्य है :
भक्तिकाल का काल विभाजन :
1. निर्गुण धारा : (क) ज्ञानाश्रयी शाखा (संत काव्यधारा) – इसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं ।
(ख) प्रेममार्गी शाखा ( सूफ़ी काव्यधारा) – इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं ।
2.सगुण धारा : (क) रामभक्ति शाखा – इसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं ।
(ख) कृष्णभक्ति शाखा – इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं ।
इस प्रकार कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्तर्गत संत-काव्य धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में इन महाकवियों का आविर्भाव हुआ था, संभवत: इसी को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ ‘द मॉडर्न वर्नाक्यूलयर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान’ (1888 ई.) में फली बार भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा ।
नामदेव द्वारा प्रवर्तित संत-काव्य-परम्परा को सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित करने का श्रेय इनको ही दिया जाता है।
उनके शिष्य धर्मदास के अनुसार कबीर का जन्म संवत् 1455 (अर्थात् 1398 ई.) में काशी में हुआ है। 120 वर्ष की दीर्घ आयु पूरी करके उनकी मृत्यु संवत् 1575 में (अर्थात् 1518 ई.) हुई।
किंवदन्ती है, कि नीरू-नीमा नामक जुलाहा दम्पत्ति ने नवजात शिशु को कहीं पड़ा हुआ पाया । उसे अपना पुत्र मानकर उसका पालन-पोषण किया। वही बालक आगे चलकर कबीर हुए। इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था ।
कपड़ा बुनने का पैतृक व्यवसाय वे आजीवन करते रहे। साधु-सन्तों की संगति उन्हें बचपन से ही प्रिय थी। हिन्दू-मुसलमान का भेद-भाव उनके मन में नहीं था। कबीर रामानंद के शिष्य थे। परंतु कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे ।
कबीर ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। अपने को कवि घोषित करना उनका उद्देश्य भी नहीं था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य धर्मदास ने कबीर वाणी का संकलन ( उनके उपदेशों का संकलन) ‘बीजक’ (1464 ई.) के नाम किया । इस ग्रंथ के तीन भाग है- रमैनी साखी और सबद । ये रचनाएँ कबीर ग्रंथावली में संगृहीत हैं।
कबीर ने बाह्याडम्बरों का विरोध किया है। उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। उनके राम सर्वव्यापी हैं।
कबीर जी एक कवि, भक्त और सुधारक के रूप में सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं शोषण की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने माया का विरोध किया है।
कृपया इसे भी पढ़ें : नीति काव्य किसे कहते हैं ?
कबीर की कविता के मुख्यत: तीन विषय है- प्रताड़ना, उपदेश और स्वानुभूति चित्रण। इन तीनों में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है। परमात्मा की भक्ति में जात-पाँत का भेद, ऊँच-नीच का भाव, रूढ़ियों का अनुसरण, मूर्ति पूजा, तिलक-चन्दन, रोजा-नमाज आदि के लिये फटकारना उनके संत स्वभाव का द्योतक है। उनकी भर्त्सना में उपदेश का भाव है।
कबीर के उपदेश सम्बन्धी पदों में जीवन की दार्शनिकता भरी हुई है। उनमें गुरु-महिमा, ईश्वर-महिमा, प्रेम-महिमा, सत्संग-महिमा, माया का फेर आदि का सुन्दर वर्णन मिलता है।
कबीर के काव्य में रहस्यवादी भावना मिलती है। वे आत्मा को दुल्हन और परमात्मा को प्रियतम मानते हैं। वे गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं।
कबीर घुमक्कड़ संत थे। जगह-जगह साधु सन्तों के सम्पर्क में वे रहे थे। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी भाषा अर्थात् राजस्थानी-पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को सधुक्क्ड़ी कहा है ।
श्यामसुंदर दास ने खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है ।
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है – “भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी इसमें संदेह नहीं ।
कबीर अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे। सरलता, सुबोधता और स्पष्टता उनकी शैली की विशेषताएँ है। उनकी शैली में उलटबासियाँ और अन्योक्तियाँ भी मिलती हैं।
कबीर को छन्दों का ज्ञान नही था, परन्तु छन्दों की स्वच्छन्दता ही कबीर की काव्य की सुन्दरता बन गई है।
अलंकारों का चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति कबीर में नहीं थी, पर उनका स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुग्ध कर लेता है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक अनुप्रास, विरोधाभास आदि अलंकारों के सुन्दर प्रयोग हुए हैं।
कबीर की भाषा में अभिव्यक्ति के सभी आवश्यक सूत्र उपलब्ध हैं। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा है –“भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे ।”
कबीर भक्त पहले और कवि बाद में थे। वे पढ़े लिखे नहीं बहुश्रुत थे। ‘मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी’ उनका मूलमंत्र था।
उनकी कविता में सच्चे गुरु का भी गौरव गान मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य का सर्वाधिक महत्व धार्मिक एवं सामाजिक एकता और भक्ति का सन्देश देने में हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, “हिन्दी साहित्य के एक हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ।”
कबीर का समाज दर्शन
कबीरदास का जन्म ऐसे समय में हुआ, जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का बोलबाला था और हिन्दू-मुसलमान आपस में दंगा-फसाद करते रहते थे। धार्मिक पाखण्ड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के ठेकेदार अपने स्वार्थ की रोटियां धार्मिक कट्टरता एवं उन्माद के चूल्हे पर सेंक रहे थे। कबीर ने इसका डटकर विरोध किया और सभी क्षेत्रों में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने अपनी बात निर्भीकता से कही तथा हिन्दुओं और मुसलमानों को डटकर फटकारा।
वस्तुतः कबीर भक्त और कवि बाद में थे, वे सही अर्थों में समाज-सुधारक पहले थे। उनकी कविता में समाज-सुधार की जो भावना मिलती है, उसे निम्न शीर्षकों में समझाया जा सकता है, समाज सुधार की यह भावना ही उनके समाज दर्शन को अभिव्यक्त करती है।
धार्मिक पाखण्ड का खण्डन
कबीर स्वच्छन्द विचारक थे। वे मानवतावादी आस्था के साथ समाज में सुधार लाना चाहते थे। अतः उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में जहाँ भी कहीं प्रगति को रोकने वाली रूढ़ियां देखीं, वहीं उनका डटकर खण्डन किया तथा बाहरी आडम्बरों को बढ़ावा देने वाले सभी धर्मों की खुलकर आलोचना की। धर्म के ठेकेदार बनने का दम्भ करने वाले पण्डे-पुजारियों, ढोंगी साधु-फकीरों तथा मुल्लाओं को कबीर ने खूब फटकारा।
वास्तव में समाज-सुधार और मानव-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने काव्य रचना की और इसे अपना अस्त्र बनाया। कबीर ने हिन्दू-मुसलमानों दोनों के पाखण्डों का खण्डन किया तथा उन्हें सच्चे मानव-धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दोनों को कसकर फटकारा। हिन्दुओं से कहा कि तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो अपना घड़ा किसी को छूने नहीं देते, किन्तु तब तुम्हारी उच्चता कहाँ चली जाती है जब वेश्यागमन करते हो ?
हिन्दू अपनी करें बड़ाई, गागरि छुअन न देई।
वेश्या के पायन तर सोवें यह देखो हिन्दुआई।।
कबीर ने मुसलमानों के पाखण्ड का भी खण्डन जोरदार शब्दों में करते हुए कहा :
कांकर-पाथर जोरि कै मसजिद लई चुनाय।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाया।
लोग मस्जिद पर चढ़कर जोर-जोर से अजान देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ईश्वर बहरा नहीं है, उसे आडम्बर प्रिय नहीं है।
वे कहते हैं :
ना हम पूजें देवी-देवता, न हम फूल चढ़ाई।
ना हम भूरत धरें सिंहासन ना हम घण्ट बजाई।।
उन्होंने हिन्दू ही नहीं, मुसलमानों द्वारा मस्जिद में चिल्ला-चिल्लाकर खुदा को पुकारने का विरोध किया उन्होंने सच्ची बात यही बताई कि:
मोकों कहाँ ढूंढ़े बन्दे, मैं तो तेरे पास में।
ना मन्दिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलास में।।
मूर्ति-पूजा का विरोध
कबीर ने मूर्ति-पूजा का खण्डन किया और मन मन्दिर में ही ईश्वर का निवास बताया। उन्होंने मूर्ति-पूजा तथा उसके आडम्बरों को स्पष्ट रूप से नकारा तथा कहा :
पाहन पूजैं हरि मिलें तौ मैं पूजूं पहार।
घर की चाकी कोई न पूजै पीसि खाय संसार।। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगूं। यह सब ढोंग है। इससे अच्छा तो यह है कि हम घर की उस चक्की को पूजें जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं। वह हमारे उपयोग की वस्तु तो है।
यही नहीं वे दुनिया के इस बावलेपन का उपहास इन शब्दों में करते हैं :
दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाय।
घर की चकिया कोई न पूजै जेहि का पीसा खाया।
बाह्याडम्बरों का खण्डन
कबीर रूढ़ियों एवं आडम्बरों के सतत विरोधी रहे। उन्होंने रोजा, नमाज, छापा, तिलक, माला, गंगास्नान, तीर्थाटन आदि का मुख्य विरोध किया। वे कहते हैं:
माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर।
करका मनका डारि के मन का मनका फेर।।
कबीर कहते हैं कि इस बाह्याचार में क्या रखा है। हिन्दू अपने देवताओं को पूज-पूज कर मर गए, मुसलमान हज यात्रा कर-करके मर गए, योगी जटाएं बांधकर मर गए, परन्तु इनमें से राम किसी को नहीं मिला :
देव पूजि हिन्दू मुये तुरक मुये हज जाई।
जटा बांधि योगी मुए, राम किनहू नहिं पाई।।
निश्चय ही कबीर निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें जो अच्छा लगा, उन्होंने निडर होकर एवं निस्संकोच होकर कहा।
समाज के प्रति जागरूक कबीर ने साधना के क्षेत्र में व्याप्त बाह्याडम्बरों का डटकर विरोध किया। लोग बाह्याचारों को ही धर्म समझकर आन्तरिक शुद्धता पर बल नहीं देते यह बात कबीर को पता थी इसलिए उन्होंने जनता को सचेत करते हुए कहा कि जटा होना, केशलुंचन, मौन व्रत, सिर मुण्डन, तिलक मुद्रा, हज यात्रा से कोई साधक नहीं हो जाता। लोग तन का योग साध रहे हैं, जबकि उन्हें मन का योग साधना चाहिए।
छुआछूत का विरोध
कबीर ने अपने समय में फैली छुआछूत की भावना का तीखा विरोध किया है। वे जाति-प्रथा के कट्टर निन्दक थे। वे कहते हैं :
जो तू बाँभन बांभनी जाया, आन बाट व्है क्यों नहिं आया?
इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों से भी प्रश्न किया है :
जो तू तुरक तुरकिनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया?
कबीर का युग सामाजिक विश्रृंखलता का युग था। ब्राह्मण वर्ग जाति अभिमान से ग्रस्त था। अपने को ऊँचा एवं शूद्रों को नीचा मानकर उन्होंने समाज में जो छुआछूत की प्रथा चला रखी थी उसका कबीर ने तीव्र विरोध किया। वे कहते हैं कि ऊँचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊँचा नहीं हो जाता। ऊँचा वह है जिसकी करनी अच्छी हो। स्वर्ण कलश यदि मदिरा से युक्त है तो निन्दनीय है :
ऊँचे कुल का जनमिया करनी ऊँच न होय।
सुबरन कलस सुरा भरा साधू निन्दत सोय ।।
कबीर प्रश्न करते हैं कि जब हमारे शरीर की नसों में एक जैसा रक्त प्रवाहित हो रहा है तो आप ब्राह्मण और हम शूद्र कैसे हो गए :
हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूद।
तुम कैसे बांभन पाण्डे हम कैसे सूद?
अवतारवाद का खण्डन
कबीर ने अवतारवाद का खण्डन किया। वे जानते थे कि अवतारवाद के नाम पर पण्डे-पुरोहित जनता को ठग रहे हैं। वे ‘राम’ को दशरथ पुत्र न मानकर निर्गुण ब्रह्म मानते हैं :
दसरथ सुत तिहूं लोक बखाना।
राम नाम का मरम है आना।।
हिंसा का विरोध
कबीर ने हिंसा का विरोध हर स्तर पर किया चाहे वह जीभ के स्वाद के लिए की गई हो, या धर्म के नाम पर की जा रही हो। मुसलमान दिन में रोजा रखते हैं और रात को गाय की कुर्बानी देते हैं। ये दोनों विरोधी कार्य हैं, इससे भला खुदा प्रसन्न कैसे हो सकता है :
दिन में रोजा रहत है राति हनत है गाय।
यह तौ खून वह बंदगी कैसे खुसी छुदाय।।
गाय तो हमारी माता जैसी है। यह हमें दूध पिलाती है, उसका वध तो माता के वध जैसा है:
जाको दूध धाइ करि पीजै।
ता माता कौ वध क्यूं कीजै।।
वे कहते हैं कि हिंसा का परिणाम भी बुरा होता है। बकरी तो केवल पत्तियां खाती है, इस पाप कर्म के कारण उसकी खाल खींची जाती है, किन्तु जो मनुष्य बकरी को खाते हैं उनका क्या हाल होगा?
बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल।
जे नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल।।
पुस्तकीय ज्ञान का खण्डन
कबीर शास्त्र ज्ञान पर नहीं आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। जो शास्त्र का पण्डित होने के आधार पर समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, कबीर उनके विरोधी हैं। काजी से वे कहते हैं :
काजी कौन कतेब बखाने।
पढ़त-पढ़त केते दिन बीते, गति एकै नहिं जानै।।
इसी प्रकार ‘शास्तर’ के पण्डित को चुनौती देते हुए वे कहते हैं :
तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आंखिन की देखी।
मैं कहता सुरझावन हारी तू राखा उरझोय रे।॥
कबीर सदाचरण पर बल देते हैं, शास्त्र ज्ञान पर नहीं। लोगों की कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिए।
कंचन और कामिनी का विरोध
कबीर ने कंचन और कामिनी को साधना के मार्ग में बाधक बताया है। उनका विश्वास रहा है कि नारी मनुष्य को अध्यात्म या सुधार के मार्ग पर चलने से रोकती है। यह बात भी तत्कालीन आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में समझी जानी चाहिए। वास्तव में वे नारी के माध्यम से अतिशय वासना की निन्दा करते हैं :
नारी की झांई परत, अन्धे होत भुजंग।
कबिरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी संग।।
कंचन और कामिनी को कबीर ने अग्नि के समान प्राणनाशक बताते हुए कहा है कि :
एक कनक अरु कामिनी, दोऊ अगनि की जाल।
देखैं ही तन प्रज्वलैं, परस्या है पैमाल ।।
कुसंगति, कपट और द्वेष की निन्दा
समाज-सुधार की दृष्टि से कबीर ने कुसंगति, कपट और द्वेष की निन्दा की है। इन चीजों को अध्यात्म और व्यावहारिक दोनों प्रकार के जीवन में उन्नति में बाधक बताया है। इनको एकदम त्यागने की बात कही है। कुसंगति पर एक उक्ति द्रष्टव्य है:
मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराइ।
कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहूं भाइ।।
इस प्रकार कपट के विषय में भी कही गई पंक्तियां द्रष्टव्य हैं :
कबीर वहाँ न जाइए, जहाँ कपट का हेत।
जानूं कली कनेर की तन रातौ मन सेत ।।
सदाचरण पर बल
कबीर ने सदाचरण पर बल दिया है। उनका मत है कि अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए तथा बुरी बातों का त्याग करना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य रहे तो ठीक है :
साधू ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय।
सार-सार को गहि रहे थोथा देई उड़ाइ।।
कबीर अपने युग के प्रति पूर्ण सचेत थे। सत्य पर वे विशेष बल देते हुए कहते हैं :
सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप।
जाके हिरदय सांच है ताके हिरदय आप।।
भले ही हम ठग लिए जाएं, किन्तु दूसरे को कभी न ठगें यही कबीर के जीवन का आदर्श है।
राम-रहीम की एकता पर बल
कबीर ने राम-रहीम, केशव, महादेव और मोहम्मद की एकता पर बल दिया। उन्होंने सम्पूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है :
दुइ जगदीश कहाँ ते आया, कहु कौनै भरमाया।
कबीर ने समझाया कि हिन्दू-तुरक दोनों का एक ही मार्ग है :
हिन्दू तुरक की एक राह है सतगुरू यहै बताई।
निष्कर्ष
इस प्रकार कबीर एक महान् समाज-सुधारक, सत्य धर्म के प्रतिपादक, समन्वयवादी तथा क्रांतिदर्शी थे। वे समाज में प्रचलित प्रत्येक प्रकार की असमानता, बाह्याडम्बर और ढोंग को समाप्त कर देना चाहते थे। यह काम स्पष्टवक्ता, दृढ़-विवेकी और निर्भीक व्यक्ति ही कर सकता है। कबीर को किसी का भय नहीं था। वे तो घर फूंककर तमाशा देखने वालों में थे। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही कुछ निर्माण कर सकता है। तभी तो कबीर की घोषणा थी कि :
कबिरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ।
जो घर फूंके आपणा, चलै हमारे साथ।।
निश्चय ही कबीर का व्यक्तित्व क्रान्तिकारी चेतना से युक्त था। उन्होंने अपने समय में निर्भीकतापूर्वक समाज सुधार का जो प्रयास किया वह अद्वितीय है। वर्तमान युग के तथाकथित समाज सुधारक भी ऐसा साहस नहीं दिखा सकते जो कबीर ने धार्मिक उन्माद से ग्रस्त तत्कालीन युग में दिखाया था। एक सच्चे
युगपुरुष की भांति उन्होंने अन्धविश्वासों, रूढ़ियों, अनीति-अनाचारों एवं दोषों पर प्रबल प्रहार करते हुए समाज को सही दिशा निर्देश देने का प्रयास किया। निश्चय ही ऐसा करके उन्होंने अपने गम्भीर दायित्व का निर्वहन किया है। इसमें उन्हें कहाँ तक सफलता मिली इसका निर्णय तो विद्वान इतिहास लेखक ही कर सकते हैं।

नमस्कार ! मेरा नाम भूपेन्द्र पाण्डेय है । मेरी यह वेबसाइट शिक्षा जगत के लिए समर्पित है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और अनुवाद विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य है । मैं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ।
मेरे लेक्चर्स हिंदी के छात्रों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं ।
मेरी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है : बीएससी, एमए (अंग्रेजी) , एमए (हिंदी) , एमफिल (हिंदी), बीएड, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन (गोल्ड मेडल), यूजीसी नेट (हिंदी), सेट (हिंदी)
मेरे यूट्यूब चैनल्स के नाम : Bhoopendra Pandey Hindi Channel, Hindi Channel UPSC