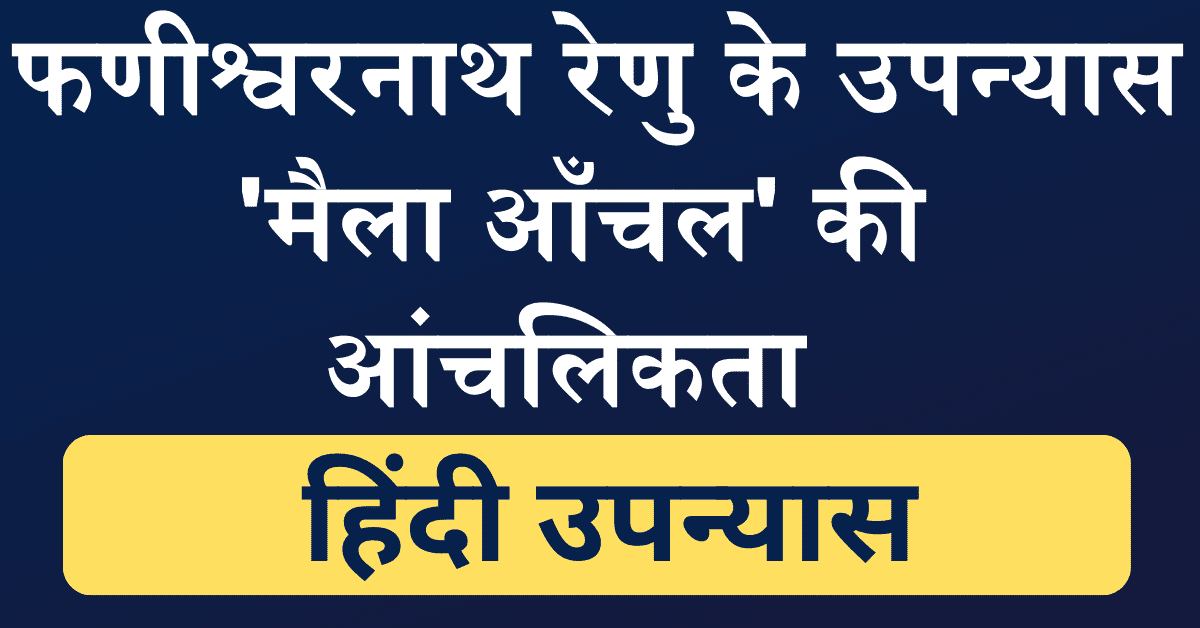फणीश्वरनाथ रेणु जन्म 4 मार्च, 1921 को औराही हिंगना नामक गाँव, जिला पूर्णिया (बिहार) में हुआ था । आपका देहावसान 11 अप्रैल, 1977 को हुआ ।
फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख कृतियाँ
संस्मरण : ऋणजल धनजल, वन तुलसी की गन्ध, समय की शिला पर, श्रुत-अश्रुत पूर्व
रिपोतार्ज : नेपाली क्रान्ति-कथा (रिपोर्ताज़);
रेणु रचनावली (समग्र)
मैला आँचल के प्रथम संस्करण की भूमिका
9 अगस्त, 1954 को मैला आँचल के प्रथम संस्करण की भूमिका के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है : “यह है मैला आँचल, एक आँचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है; इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल । विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है, जब हम दक्खिन में सन्थाल परगना और पच्छिम में मिथिला की सीमा रेखाएँ खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गाँव को पिछड़े गाँवों का प्रतीक मानकर-इस उपन्यास-कथा का क्षेत्र बनाया है।”
पुन: रेणु जी लिखते हैं : “इसमें फूल भी हैं शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चन्दन भी, सुन्दरता भी है, कुरूपता भी मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया।”
“कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ; पता नहीं अच्छा किया या बुरा। जो भी हो, अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता ।”
मैला आँचल की आँचलिकता
‘मैला आँचल’ हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आँचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर-पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इसमें वहाँ के जीवन का, जिससे वह स्वयं भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यन्त जीवन्त और मुखर चित्रण किया है।
‘मैला आँचल’ का कथानायक एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक पिछड़े गाँव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है, और इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुःख-दैन्य, अभाव, अज्ञान, अन्धविश्वास के साथ-साथ तरह-तरह के सामाजिक शोषण-चक्रों में फैसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। कथा का अन्त इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम-चेतना तेजी से जाग रही है।
कथाशिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की इस युगान्तरकारी औपन्यासिक कृति में कथाशिल्प के साथ-साथ भाषा और शैली का भी विलक्षण सामंजस्य है जो जितना सहज-स्वाभाविक है, उतना ही प्रभावकारी और मोहक भी। ग्रामीण अंचल की ध्वनियों और धूसर लैंडस्केप्स से सम्पन्न यह उपन्यास हिंदी कथा-जगत में पिछले कई दशकों से एक क्लासिक रचना के रूप में स्थापित है। अब हम ‘मैला आँचल’ के वस्तु और शिल्प के दृष्टिकोण से इसकी आँचलिकता का अध्ययन और मूल्यांकन करेंगे ।
‘मैला आँचल’ का वस्तु, शिल्प और आँचलिकता
सन पचास से साथ के दशक में हिंदी उपन्यास का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे ‘आँचलिक उपन्यास’ की संज्ञा प्रदान की गई । उपन्यास को आँचलिकत कहने तथा उसके महत्व की ओर आलोचकों का ध्यान आकर्षित करने का पूरा श्रेय सुप्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी को जाता है ।
‘मैला आँचल’ फणीश्वरनाथ रेणु कृत 1954 ई. में प्रकाशित हिंदी का सुप्रसिद्ध आँचलिक उपन्यास है।
अंचल का शाब्दिक अर्थ है-जनपद या क्षेत्र। जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिम्बात्मक चित्रण होता है, उन्हें आँचलिक उपन्यास कहा जाता है ।
आँचलिक उपन्यासों का मूल उद्देश्य किसी विशिष्ट अंचल के समग्र जीवन का विस्तार से चित्रण करना होता है, अतः उसमें जनपद के भूगोल, सभ्यता, रहन-सहन, वेशभूषा, रूढ़ियां, सामाजिक परम्पराएं, लोकजीवन, त्योहार-पर्व, नृत्य-गीत, रीति-रिवाज, लोक भाषा, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, राजनीतिक चेतना, आर्थिक कठिनाइयां आदि का समावेश करता है।
रेणुजी के दो आँचलिक उपन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। इनके नाम हैं- ‘‘मैला आँचल’’ और ‘परती परिकथा’।
‘‘मैला आँचल’’ के कथानक में लेखक ने सन् 1942 ई. से लेकर गांधीजी के निधन तक की ‘मेरीगंज’ (जिला पूर्णिया, प्रान्त बिहार) के जन-जीवन और परिस्थितियों का जीवन्त चित्र प्रस्तुत किया है।
गाँव में विभिन्न वर्गों के लोग अपने-अपने ‘टोले’ में रहते हैं। मेरीगंज एक पिछड़ा हुआ गाँव है जिसमें उच्चवर्ग-निम्नवर्ग, धनी-निर्धन, सभी वर्गों के लोग रहते हैं। इनमें पारस्परिक संघर्ष चलता रहता है।
आजादी मिलने के बाद निम्न वर्ग में नई चेतना का उदय हुआ, जिससे यह संघर्ष और भी तीव्र हो गया। इस गाँव की प्रगति में बाधक तत्व हैं- प्राचीन रूढ़िगत संस्कार, छुआ-छूत, आपसी संघर्ष, अंध-विश्वास आदि।
जनता अब अपने उन दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानने लगी। जो आजादी मिलते ही खद्दर पहनकर देशभक्ति और जनसेवा का लबादा ओढ़े हैं, किन्तु हैं पक्के स्वार्थी। यही इस उपन्यास की मूल चेतना है।
लेखक ने इस मूल चेतना का आधार गांधीवादी दर्शन को ही बनाया है जिसके कारण स्वार्थी एवं अत्याचारी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है और जमींदार अपनी सात सौ बीघा जमीन किसानों में बांटकर त्याग की जीती-जागती मूर्ति बन जाता है।
रेणुजी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इस उपन्यास में स्थान-स्थान पर किया है। ‘मेरीगंज’ का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है, “मेरीगंज एक बड़ा गाँव है; बारहों बरन के लोग रहते हैं। गाँव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है…… राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आये हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं । …….. सारे मेरीगंज में दस आदमी पढ़े-लिखे हैं – पढ़े-लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई।”
‘मैला आँचल’ यद्यपि स्वतंत्रता के उपरान्त प्रकाशित हुआ किन्तु इसमें स्वतंत्रता पूर्व का परिवेश प्रस्तुत किया गया है। गाँव की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि मलेरिया सेन्टर गाँव में खुलने का विरोध अधिकतर ग्रामीण करते हैं। गाँव का ज्योतिषी पण्डित गाँव वालों को इस अस्पताल के विरुद्ध भड़का देता है क्योंकि अस्पताल खुलने से उसे आर्थिक हानि हो रही थी।
डाक्टर प्रशांत को गाँव में आकर जो अजीबो-गरीब अनुभव होते हैं, वे उस अंचल के पिछड़ेपन का दस्तावेज हैं। समूचा अंचल अंधविश्वास, शोषण, संघर्ष, निर्धनता, अशिक्षा से ग्रस्त है।
इस उपन्यास के कुछ पात्र – बलदेव, बावनदास, कालीचरण-अपने-अपने ढंग से संघर्ष करते दिखाये गये हैं। उपन्यास के अन्त में बावनदास अपना बलिदान देकर पाठकों को अपने चरित्र से प्रभावित करता है।
‘मैला आँचल’ की कथा और उसके पात्र अंचल विशेष तक सीमित रहे हैं परन्तु वर्णनात्मक प्रसंगों की अधिकता के कारण कथा-संगठन में शिथिलता आ गई है। पात्रों में भी स्वाभाविकता दिखाई नहीं पड़ती।
लेखक ने नई उभरती जनचेतना का मार्मिक चित्रण करते हुए यह संकेत दिया है कि भारत के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण यह जनचेतना करेगी।
‘मैला आँचल’ में अंचल विशेष को समग्रता से देखने का आग्रह है। अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने आँचलिक शब्दावली, लोकोक्तियों, मुहावरों का उपयोग किया है। लेखक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति विशेष आग्रहशील दिखाई पड़ता है। आँचलिकता को उभारने के लिए रेणुजी ने अंचल की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक बनावट पर ध्यान केन्द्रित किया है।
कृपया इसे भी पढ़ें : राग दरबारी उपन्यास की भाषा-शैली
रेणुजी ने इसमें गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप पात्रों का हृदय परिवर्तन दिखाया है जो कहीं-कहीं अस्वाभाविक प्रतीत होता है। शोषक मानसिकता वाले तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का हृदय परिवर्तन स्वाभाविक नहीं लगता।
वस्तुतः ‘मैला आँचल’ अपने युग का जीवन्त यथार्थ है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज जैसे गाँव ही सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हैं, मेरीगंज की समस्याओं के बहाने वे सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्याओं को व्यक्त करने का प्रयास करते जान पड़ते हैं।
‘मैला आँचल’ में तत्कालीन राजनीति, नेताओं की अवसरवादिता, स्वार्थवृत्ति, सिद्धान्तप्रिय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आदि का ययार्थ चित्रांकन किया गया है। इसमें एक ओर घोर हिन्दूवादी पार्टी के लोग हैं जो असहिष्णु हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस के बलदेव जी हैं जो हिंसा का हर हाल में विरोध करते हैं। तपे हुए कार्यकर्ता बावनदास के लिए आजादी के बाद कांग्रेस में कोई जगह नहीं है क्योंकि अब अवसरवादी स्वार्थी नेताओं की बन आई है।
रेणु ने बड़ी सफाई से उपन्यास में यह दर्शाया है कि गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन जिन जीवन मूल्यों के आधार पर किया था वे आजादी मिलते ही नेताओं की दृष्टि में अप्रासंगिक होने लगे तथा चारों ओर सिद्धान्तहीन, स्वार्थी, अवसरवादी नेताओं की तूती बोलने लगी।
उपनिवेशवाद के शोषण उत्पीड़न के साथ-साथ सामंतवादी शक्तियों द्वारा जनता के शोषण को भी ‘मैला आँचल’ में कथानक की विषय वस्तु बनाया गया है।
कालीचरण और चलित्तर के चरित्र यह संदेश देते हैं कि सफल न होने पर अहिंसक क्रांति प्रतिशोध रूप में हिंसक रूप धारण कर लेती है। नक्सलवाद इसी की परिणति है।
‘मैला आँचल’ भले ही आँचलिक उपन्यास होने के कारण अंचल विशेष तक सीमित रहा है किन्तु इसका कथानक राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे मूल्य संक्रमण, अवमूल्यन एवं नकारात्मक परिवर्तनों को पूरी तरह उजागर करता है।
‘मैला आँचल’ में उपन्यासकार ने ‘दृश्यात्मक’ एवं ‘परि- दृश्यात्मक’ दोनों शिल्प प्रविधियों का प्रयोग किया है। दृश्यात्मक विधि में दृश्य और पाठक के बीच उपन्यासकार नहीं होता, पाठक स्वयं दृश्य का अवलोकन करता है जबकि परिदृश्यात्मक विधि में उपन्यासकार पाठक को दृश्य दिखाता है।
‘मैला आँचल’ में पूर्णिया में जो रैली आयोजित की गई है, उसका चित्रण दृश्यात्मक विधि से लेखक इस प्रकार करता है, “चलो-चलो पुरैनियां चलो। मेनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत-मर्द, बाल-बच्चा, झंडा-पत्तरव और इनकिलाब जिन्दाबाद करते हुए पुरैनियां चलो।……. रेलगाड़ी का टिकस ।……. कैसा बेकूफ है! मैनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा?”
यहाँ भाषा का रूप उल्लेखनीय है। पूर्णिया को ‘पुरैनियां’ मिनिस्टर को ‘मेनिस्टर’, ‘टिकट’ को ‘टिकस’, ‘बेवकूफ’ को ‘बेकूफ’ कहकर ग्रामीण अंचल में प्रयुक्त तद्भव शब्दावली का सुन्दर चित्रण किया गया है।
ग्रामीणों की सोच भी देखिए, जब मिनिस्टर साहब की रैली है तो टिकट की क्या आवश्यकता है, कौन टिकट मांगेगा, अतः बेटिकट चलना है। आज की रैलियों में भी कमोवेश यही स्थिति रहती है।
पूर्वदीप्ति पद्धति का प्रयोग भी इस उपन्यास में किया गया है। प्रशान्त की कथा पूर्वदीप्ति के माध्यम से ही प्रस्तुत की गई है।
ग्रामीण संस्कृति को लोकगीतों, लोकधाओं के माध्यम से व्यक्त करने में रेणुजी को सफलता मिली है। सुराजी कीर्तन का एक स्वरूप निम्नलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है :
“कथि जे चढ़िये आयेल
भारथमाता
कथि जे चढ़ल सुराज
चलु सखी देखन को !
कथि जे चढ़िये आयेल
बीर जमाहिर
कथि पर गंधी महाराज।।“
अर्थात् ‘भारतमाता’ किस वाहन पर सवार होकर आयी हैं और ‘स्वराज्य’ किस वाहन पर सवार है ? वीर जवाहरलाल किस वाहन पर सवार होकर आए हैं और महात्मा गांधी महाराज किस वाहन पर सवार हैं?”
‘मेरीगंज’ सम्पूर्ण देश के राजनीतिक वातावरण का नमूना प्रस्तुत करता है। यहाँ के राजनीतिक दल देश सेवा के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे थे। उनका प्रयास दूसरे दलों को नीचा दिखाने की ओर केन्द्रित था।
जमींदार और अधिकारियों के अत्याचार सहने को जनता विवश थी। असामियों को अब भी जूतों से पिटवाया जाता था। भले ही जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई हो किन्तु वे पुलिस, पटवारी से मिलकर रिश्वत के बल पर अपनी शक्ति और सत्ता बनाये हुए थे।
संथालों को मारा-पीटा गया और उनकी जमीन भी छीन ली गई। उनके टोले को लूट लिया गया। चुनाव के समय जातिवाद हावी रहता था। चुनाव पैसे के बल पर लड़े और जीते जाते थे।
बावनदास कहता है, “यह पटनियां रोग है। किसका आदमी ज्यादा चुना जाय, इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी के लोग ज्यादा आए तो सबसे बड़ा मंत्री भी राजपूत का होगा। जितने बड़े लोग हैं, मंत्री बनने के लिए मार कर रहे हैं।”
निष्कर्ष
लेखक ने तटस्थ भाव से उस अंचल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है। जनता भले ही अशिक्षित हो किन्तु स्वार्थपरायण लोगों की स्वार्थपरता को समझ ही लेती है। वास्तव में इस उपन्यास का नायक कोई पात्र न होकर ‘अंचल’ है।
‘मैला आँचल’ में ‘रेणु’ जी का चिन्तन प्रगतिशील है और वे जनसाधारण के समर्थक हैं। वे सामंतवादी व्यवस्था के पक्षधर नहीं हैं और उभरते पूंजीवाद की विकृतियों का यथातथ्य चित्रण करते हुए पाठकों के मन में पूंजीवाद के प्रति वितृष्णा उत्पन्न कर देने में सक्षम हैं।
रेणुजी गरीब के पक्षधर बनकर सामने आए हैं। ‘मैला आँचल’ में चित्रित गरीब किसानों, मजदूरों, संथालों के संघर्ष को उन्होंने अपना समर्थन दिया है और इस प्रकार मुंशी प्रेमचन्द के ‘आदर्शोन्मुख यथार्थवाद’ को आगे बढ़ाया है।
उनका एक पात्र प्रशान्त कहता है कि “मैं यहाँ प्यार की खेती करना चाहता हूँ” यह संकल्प काल्पनिक नहीं है। इसके माध्यम से वे ग्राम सुधार के तमाम प्रयासों को अपना समर्थन देते दिखाई पड़ते हैं।
विश्वनाथ प्रसाद का हृदय परिवर्तन ‘मैला आँचल’ की एक महत्वपूर्ण घटना है।
कालीचरण जैसे युवकों के नेतृत्व में ग्राम सुधार सम्पन्न होगा यह रेणूजी की दृढ़ धारणा है।
निश्चय ही रेणूजी की दृष्टि व्यापक जनतान्त्रिक मूल्यों पर टिकी है और वे चाहते हैं कि ग्रामीण भारत में भी विकास की गंगा बहे।
मेरीगंज में कबीर पंथियों का एक मठ है जहाँ साधु रहते हैं। ‘मैला आँचल’ में साधुओं का प्रतिनिधित्व यहाँ रहने वाला साधु करता है जो बिना गाली के बात नहीं करता।
उसकी भाषा का नमूना देखिए-आते ही लक्ष्मीदासिन पर बरस पड़े, “तेरी जात को मच्छड़ काटे हरामजादी रंडी। तैं समझती क्या है री। तैं आचारज गुरु को गाली देती है ? तेरे मुंह में कुल्हाड़ी का डंडा डाल दूं बोल! साली कुत्ती साधू का रगत बहाती है और बाबू लोग से मुंह चटवाती है। अभी तेरे गाल पर चांटा, हट जा यहाँ से कातिक की कुतिया।”
उदाहरण के लिए ‘मैला आँचल’ की भाषा में प्रयुक्त कुछ आँचलिक शब्द इस प्रकार हैं – जायहिन्द, आन्दोलन, विदमान, महातमा, इसबिस जमाहिरलाल, रजीन्नर बाबू, टीपते, सुराज, डिस्टीबोट, सास्तर, सितलमंटी, मूलगैन, ठेठर, लैन, निपुत्तर, संघटन, इस्पाट, लाटबंदी, बराह छत्तर, चुमौना, बिलटा, तालपता, रहस रौण्ड, अकलंग।
भाषा में पात्रानुकूलता का गुण भी विद्यमान है। राजनीतिक नेता अपने भाषणों में परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग करते हैं और बीच-बीच में अंग्रेजी के शब्द भी बोलते हैं।
स्थानीय भाषा का प्रयोग करने से उपन्यास में आँचलिकता पूरी तरह उभर कर सामने आयी है। लोक भाषा का प्रयोग वातावरण का यथातथ्य चित्रण करने में तथा पात्रों के संवादों में किया गया है। प्रकृति चित्रण और भौगोलिक विवरणों ने आँचलिकता को गहरा कर दिया है।
पात्रों के चरित्रांकन में कहीं-कहीं रेणु जी ने आवश्यकता से अधिक आदर्शवाद दिखाया है। डॉ. प्रशान्त ऐसे ही आदर्शवाद के अतिरेक से गढ़े हुए पात्र हैं, अतः पाठकों को वे कहीं-कहीं अस्वाभाविक एवं अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं।
ग्रामीण उत्सवों का वर्णन भी अधिक मात्रा में होने के कारण उपन्यास की कथा बोझिल हो गई है। यह ठीक है कि रेणुजी की अपनी ‘जीवन दृष्टि’ उपन्यास में सर्वत्र परिलक्षित होती है तथापि गाँव की सांस्कृतिक बुनावट को चित्रित करने पर उनका ध्यान अधिक केन्द्रित रहा है परिणामतः कथा में व्याघात एवं औपन्यासिकता को आघात लगा है। इस सबके बावजूद भी निश्चय ही वस्तु और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से रेणुजी का ‘मैला आँचल’ एक सफल आँचलिक उपन्यास माना जा सकता है।

नमस्कार ! मेरा नाम भूपेन्द्र पाण्डेय है । मेरी यह वेबसाइट शिक्षा जगत के लिए समर्पित है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और अनुवाद विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य है । मैं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ।
मेरे लेक्चर्स हिंदी के छात्रों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं ।
मेरी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है : बीएससी, एमए (अंग्रेजी) , एमए (हिंदी) , एमफिल (हिंदी), बीएड, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन (गोल्ड मेडल), यूजीसी नेट (हिंदी), सेट (हिंदी)
मेरे यूट्यूब चैनल्स के नाम : Bhoopendra Pandey Hindi Channel, Hindi Channel UPSC