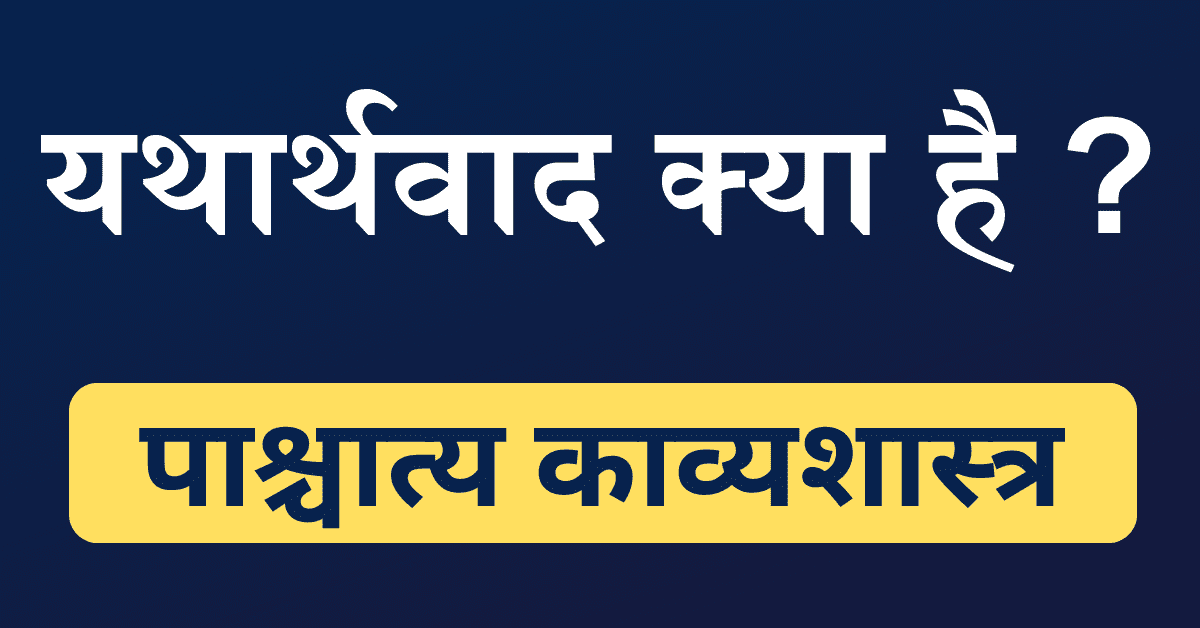हिंदी में यथार्थवाद अंग्रेजी के रियलिज्म (Realism) के अनुवाद के रूप में प्रयुक्त होता है । यथार्थ का अर्थ है यथा + अर्थ यानी जैसा है वैसा अर्थ। किंतु इसका पारिभाषिक अर्थ समझने के लिए इतिहास और दर्शन के क्षेत्र में जाना पड़ेगा ।
यथार्थवाद मूलतः दर्शन के क्षेत्र का शब्द है, जहाँ से साहित्य व कला के क्षेत्र में ले लिया गया है । इस शब्द को दर्शनशास्त्र के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम दार्शनिक प्लेटो थे ।
कला और साहित्य के क्षेत्र में ‘यथार्थवाद’ एक आंदोलन के रूप में 19 वीं सदी में फ्रांस में उभरा । 1826 में मर्क्यू फ्रांसे ने ‘यथार्थवाद’ की परिभाषा अपने निबंध में की ।
तदुपरांत 1855 में फ्रांस के प्रसिद्ध चित्रकार कूर्वे ने अपने चित्रों में यथातथ्य शैली का व्यवहार किया तथा अपनी चित्र प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर ‘यथार्थवाद’ शब्द अंकित किया ।
चित्रकला में यथार्थवाद के अभ्युदय के बाद 1857 में फ्रांसीसी उपन्यासकार ‘फ्लौबेयर’ (Gustave Flaubert) का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास ‘मदाम बोवारी’ (Madame Bovary) प्रकाशित हुआ । इस प्रकार 1855 तक फ्रांसीसी कला और साहित्य-जगत में यथार्थवाद का प्रवेश हो चुका था ।
यथार्थवादी आंदोलन सर्वप्रथम फ्रांस में आरंभ हुआ और सन् 1850-1865 के बीच अपने चरम उत्कर्ष तक पहुँच गया। जब (1857) पहली बार ‘फ्लौबेयर’ का उपन्यास ‘मदाम बोवारी’ निकला तो उसे यथार्थवाद की (और आगे चलकर उतनी ही प्रकृतिवाद की) विजय माना गया । एक और यथार्थवादी उपन्यास गोनकूर-बंधुओं का ‘यर्मिनी लांसर्ता’ (1865) था ।
यथार्थवादी विचारधारा के अभ्युदय की पृष्ठभूमि
यथार्थवादी विचारधारा के अभ्युदय की पृष्ठभूमि में दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आदि कई प्रकार के कारण रहे हैं । विज्ञान ने मानव समाज की पुरातन रूढ़ियों को तोड़कर मनुष्य का दृष्टिकोण तथ्यवादी बनाया । डार्विन के विकासवादी सिद्धांत ने मनुष्य जीवन का विकास अन्य जीव-जंतुओं की भांति मानकर मानव जीवन संबंधी धार्मिक मान्यताओं को झकझोर डाला, परिणामतः 19 वीं सदी के मनुष्य का दृष्टिकोण आदर्शवादी आवरण को भेदकर जीवन के स्थूल तथ्यों की ओर उन्मुख हुआ ।
इसके साथ ही फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत ने लोगों का ध्यान जैविक आवश्यकताओं की जरूरतों और तज्जन्य विद्रूपता, कुंठा, अतृप्ति, क्षोभ आदि से संबंधित मानव-जीवन की वास्तविकताओं की ओर आकर्षित किया । दूसरी ओर कार्ल मार्क्स की चिंताधारा ने पददलितों-शोषितों के जीवन संघर्ष की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट किया ।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 19 वीं सदी का यूरोपीय मस्तिष्क विचारधाराओं के विभिन्न झंझावातों से इस प्रकार झकझोर दिया गया था कि उसके समाज और धर्म संबंधी प्राचीन आदर्शवादी रोमानी सपने बिखर गए । वह अब यथार्थवादी दृष्टिकोण से ही सभी कुछ देखने-समझने लगा था । इस प्रकार धीरे-धीरे कला साहित्य के क्षेत्र में भी यथार्थवादी विचारधारा का असर बढ़ा।
यथार्थवादी आंदोलन की इस पृष्ठभूमि में जॉन लॉक (John Lock) द्वारा प्रणीत अनुभववादी (Empericist) विचारधारा का भी पर्याप्त प्रभाव रहा है । अनुभववादी दर्शन अनुभूत तथ्यों पर विशेष बल देता है । यह एक आत्मनिष्ठ यथार्थवादी दर्शन है ।
इस दर्शन से प्रभावित साहित्यकारों में देश- काल के गोचर रूपों तथा प्रतीतानुभूत रूपों के चित्रण की प्रवृत्ति का विकास हुआ ।
यथार्थ और यथार्थवाद
यथार्थ और यथार्थवाद एक दूसरे के पूरक हैं । जीवन की सच्ची अनुभूति यथार्थ है; पर इसका कलात्मक अभिव्यक्तीकरण यथार्थवाद है । यथार्थवाद का प्रयोग साहित्य में आदर्शवाद एवं स्वच्छंदतावाद के विपरीत अर्थों में किया जाता है । जो साहित्यकार मानव-जीवन एवं समाज का संपूर्ण तथा वास्तविक चित्र उपस्थित करता है और अपने साहित्य का विषय वायवी जगत् से न चुनकर वास्तविक जगत से चुनता है, वह यथार्थवादी कहलाता है ।
वस्तुतः ‘यथार्थवाद’ यथार्थ की आधारभूमि पर खड़ा किया हुआ जीवन का जीवंत चित्र है ।
कजामिया यथार्थवाद को एक पद्धति नहीं, विचारधारा मानते हैं (Realism in art is not a method but a tendency) ।
जार्ज लूकास यथार्थवादी साहित्य में समाज का यथावत् चित्रण मानते हैं, “(In Realism) that the author must honestly record
without fear or favour everything he sees around him)”
‘फ्लौबेयर’ वस्तुगत दृष्टिकोण और जीवन के सामान्य पक्षों के महत्वपूर्ण उद्घाटन को यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता मानते हैं ।
भारतीय विद्वानों में जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद को ‘जीवन के दुःख और अभावों’ का उल्लेख मानते हैं; आचार्य नंददुलारे वाजपेयी ‘यथार्थवाद’ का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु-जगत से जोड़ते हैं; शिवदान सिंह चौहान इसे ‘निर्विकल्प रूप से जीवन की वास्तविकता का प्रतिबिंब’ स्वीकार करते हैं तथा प्रेमचंद यथार्थवाद को ‘चरित्रगत दुर्बलताओं, क्रूरताओं और विषमताओं का नग्न चित्र’ मानते हैं ।
कृपया इसे भी पढ़ें : अतियथार्थवाद क्या है ?
यथार्थवादी साहित्य की : प्रवृतियाँ
किसी भी रचना को ‘आदर्शवादी’ श्रेणी में रखा जाए या ‘यथार्थवाद’ की कोटि में-इसका निर्णय करने के लिए उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करना आवश्यक है। एक यथार्थवादी रचना में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ समान्यत: होती हैं:
1. यथार्थवादी कलाकार-‘जीवन क्या है?’ का उत्तर देता है । वह ‘क्या होना चाहिए?’ की समस्या में नहीं पड़ता ।
2. यथार्थवादी रचना में अतीत और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का चित्रण अधिक होता है ।
3. यथार्थवादी रचनाओं में जीवन की असंगतियों, कटुताओं एवं विषमताओं का चित्रण होता है ।
4. यथार्थवादी रचना में परिस्थितियों का मानव पर प्रभाव बताया जाता है, जबकि आदर्शवादी में मानव परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है ।
5. यथार्थवादी केवल समस्या प्रस्तुत करता है, उसका समाधान आदर्शवादी करता है ।
6. यथार्थवादी में वैयक्तिकता अधिक होती है, जबकि आदर्शवादी में सामाजिकता ।
7. यथार्थवादी शैली में स्वाभाविकता, तीव्रता, व्यंग्यात्मकता अधिक होती है, जबकि आदर्शवादी शैली में काल्पनिकता, शिथिलता और कोमलता का वेग होता है ।
8. यथार्थवादी साहित्य में रौद्र, वीभत्स एवं शृंगार की अभिव्यक्ति अधिक होती है, जबकि आदर्शवादी में करूण, वीर और शांत की ।
निष्कर्ष
यथार्थवादी कलाकार का प्रयत्न हमेशा ही उन घटनाओं और पात्रों का प्रस्तुतीकरण होता है, जो वास्तविक जगत की प्रतिच्छाया हो । वह असम्भव, वायवी तथा अद्भुत को प्रकृति-विरुद्ध मानकर, उनके चित्रण को अनुचित समझकर अपने साहित्य से बहिष्कृत करता है ।
वह एक प्रकार से मानव-समाज और जीवन का अनासक्त और निष्पक्ष फोटोग्राफर होता है । वह कृति को व्यक्तिगत विचारों के प्रचार-प्रसार का साधन नहीं मानता, वरन जो कुछ उसके आस-पास घटित हो रहा है, उसके प्रकाशन कुछ का माध्यम मानता है ।
परंतु जीवन के यथावत चित्रण से तात्पर्य मात्र यौन-वर्जनाओं, कुत्सित जीवन की घटनाओं, छल-छद्मों से भरी कहानियों, भद्दी एवं अश्लील बातों के चित्रण से ही नहीं है । यथार्थवाद को मात्र असामाजिक यौन संबंधों, पतित जीवन की घृणित दुर्बलताओं का ही नग्न चित्र समझना, उसे न समझना अथवा संकीर्ण अर्थ में समझना है । ये सभी कुछ प्रकृतिवादी (Naturalism) साहित्य की विशेषताएं हैं, यथार्थवादी साहित्य की नहीं ।
क्योंकि ‘प्रकृतवादी साहित्यकार मनुष्य-जीवन के हीन एवं पाशविक पक्ष को ही अपने साहित्य का श्रेष्ठ कथावस्तु के रूप में स्वीकार करता है, जबकि यथार्थवादी साहित्यकार मनुष्य के आदर्श एवं दुर्बल दोनों रूपों का यथावत् चित्रण करता है ।
एक का उद्देश्य मनुष्य को समझदार पशु मानकर उसका दोष-दर्शन ही है, जबकि दूसरे का दोष और गुण-दोनों को सही रूप में प्रस्तुत करना ।
यथार्थवादी साहित्यकारों ने भाषा और शिल्प के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किए । सहज-सरल बोधगम्य भाषा और सहज शिल्प विधान यथार्थवादी साहित्य की खास विशेषताएं हैं । यही कारण है कि हिंदी की प्रगतिवादी परंपरा पर यथार्थवाद का सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है ।

नमस्कार ! मेरा नाम भूपेन्द्र पाण्डेय है । मेरी यह वेबसाइट शिक्षा जगत के लिए समर्पित है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और अनुवाद विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य है । मैं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ।
मेरे लेक्चर्स हिंदी के छात्रों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं ।
मेरी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है : बीएससी, एमए (अंग्रेजी) , एमए (हिंदी) , एमफिल (हिंदी), बीएड, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन (गोल्ड मेडल), यूजीसी नेट (हिंदी), सेट (हिंदी)
मेरे यूट्यूब चैनल्स के नाम : Bhoopendra Pandey Hindi Channel, Hindi Channel UPSC