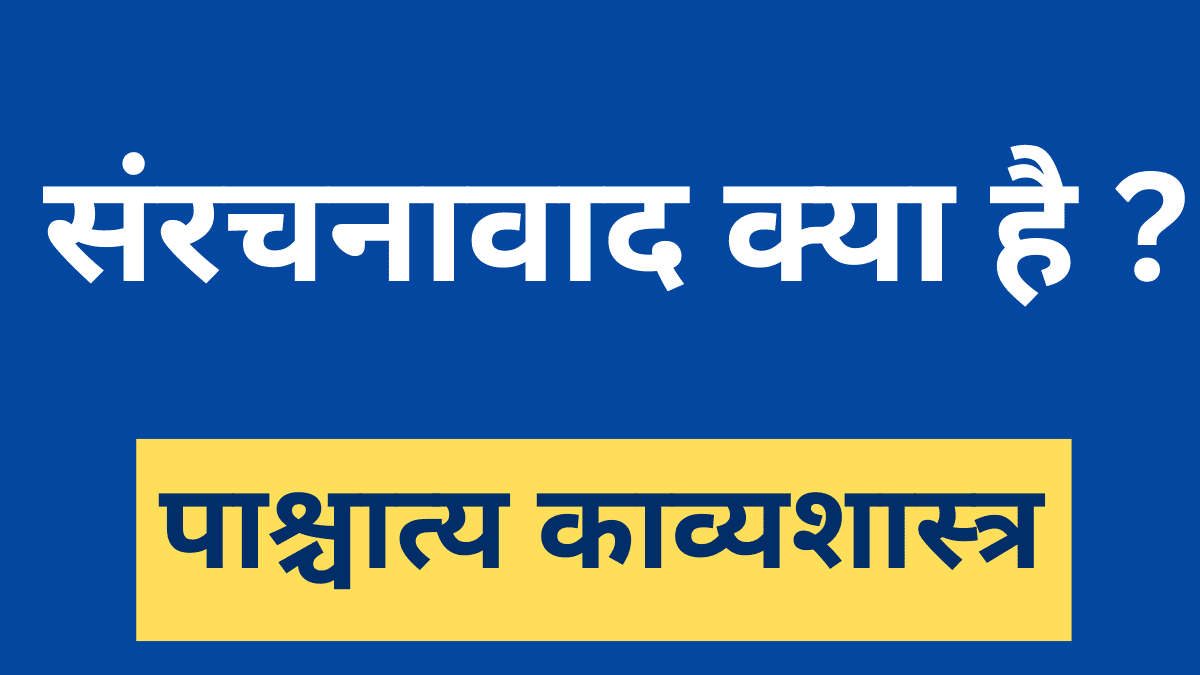संरचनावाद अंग्रेजी शब्द (Structuralism) का हिंदी पर्याय है । संरचनावाद पाश्चात्य समीक्षा जगत से हिंदी में आया। यह 1960 के दशक के फ्रांस में विकसित बौद्धिक विश्लेषण एवं चिंतन की वह पद्धति है जिसे विश्व स्तर पर भाषाविदों, साहित्य समीक्षकों, दार्शनिकों, मनोविज्ञान शास्त्रियों तथा नृविज्ञान शास्त्रियों (anthropologist) का उत्साहवर्द्धक समर्थन मिला । तो चलिए आज हम sanrachanavad kya hai को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं ।
‘संरचनावाद’ की अवधारणा का मूल स्त्रोत जेनेवा और पेरिस में भाषाविज्ञान के प्रोफेसर फर्डिनेन्ड-डि-सस्यूर (Ferdinand de Saussure, 1857-1913) द्वारा प्रतिपादित ‘भाषा-सिद्धांत’है ।‘संरचनावाद’ का केंद्रवर्ती बिन्दु ‘कृति’ है, कृतिकार अथवा समीक्षक नहीं । ‘संरचनावाद’ का गहरा संबंध ‘भाषा’ से है । ‘संरचनावाद’ भाषिक दृष्टि से साहित्य के मूल्यांकन का प्रतिमान (model) है।
भाषा का ऐसा कलात्मक प्रयोग, जो मानव स्थितियों के नाना पहलुओं को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है, ‘संरचनावाद’ के अंतर्गत आता है। भाषा और अर्थ परस्पर जुड़े रहते हैं । अतः किसी भी साहित्यिक कृति में भाषा की बनावट (Style) और बुनावट (Texture) उसकी ‘संरचना’ (Structure) से जुड़ी रहती है । इस प्रकार साहित्यिक कृतियों की भाषा की संरचना का अध्ययन उनमें नए अर्थों की खोज करता है ।
वस्तुतः ‘sanrachanavad’ का सार तत्व ‘रूपवाद’ में निहित है, जिसमें भाषा के बाहर कुछ भी अग्राह्य है । ‘रूपवाद’ ने साहित्य को रचनाकार और रचनागत परिस्थितियों से अलग कर मात्र पाठ (Text) पर बल दिया जो कालांतर में ‘संरचनावाद’ का मूल कारक बना ।
‘रूपवाद’ में भाषागत साहित्य अध्ययन पर जो बल दिया गया वही भाषाविज्ञान के संरचनावादी सूत्र के रूप में विकसित हुआ और संदेश के उद्देश्य के लिए भाषा के संरचना के प्रकार्य (Functions of language structure) को समझने के प्रयास शुरू हुए।
भाषा एक संघटक साकल्य (Organic Whole) है जिसके अनेक घटक या अवयव हैं, जैसे कि शब्द, पद, पदबंध, वाक्य, वाक्य विन्यास, इत्यादि ।
प्रत्येक अवयव एक ओर अपने अगले अवयव से जुड़ा रहता है और साथ ही अवयवी से भी। ‘संरचनावाद’ किसी वस्तु, कृति, घटना और समाज का अध्ययन इसी सावयवी पद्धति से करता है ।
उदाहरणार्थ मनुष्य एक सावयव (having organs) प्राणी है, जिसके सारे अवयव/घटक अँगुली-हाथ-पैर आदि एक-दूसरे से जुड़े हैं और साथ ही मनुष्य से भी। एक की क्षति से संरचना विखंडित हो जाएगी और एक के क्षरण का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा ।
इसके अनुसार हर वस्तु का एक अवयव, उसके अपने घटक होते हैं, उन घटकों के पारस्परिक संबंध होते हैं। प्रत्येक घटक एक ओर दूसरे घटक से सम्बद्ध होता है तो दूसरी ओर पूरे अवयवी के साथ। इसके विवेचन की एक पद्धति होती है, जिसे ‘संरचनावाद’ का नाम दिया गया है ।
‘sanrachanavad’ को पद्धति के रूप में स्थापित करने का श्रेय स्विस भाषाविद् फर्डिनेन्ड-डि-सस्यूर (Ferdinand de Saussure, 1857-1913) को जाता है । सस्यूरर ने संरचनावाद का सिलसिलेवार ब्यौरा अपनी प्रसिद्ध कृति ‘कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स (Course in General Linguistics) में दिया है ।
सस्यूर के अतिरिक्त रोमान, पॉकब्सन, लुई हेल्मस्लेव, एमिले, बेनविमिस्ते एवं चाम्स प्रमुख संरचनावादी हैं ।
संरचनावादी समीक्षक समीक्षा में रचना के उन तमाम तत्वों या अवयवों का अध्ययन करता है, जिनसे रचना अर्थ और अस्तित्व पाती है । संरचना अपने में पूर्ण होती है । उसकी पूर्णता की खोज करनी होती है । संरचना चाहे साहित्यिक कृति की हो अथवा मिथक की, पूर्णता उसकी अनिवार्यता है ।
भाषा और अर्थ परस्पर जुड़े रहते हैं । अतः किसी भी साहित्यिक कृति में भाषा की बनावट (Style) और बुनावट (Texture) उसकी संरचना (Structure) से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार साहित्यिक कृतियों की भाषा की संरचना का अध्ययन उनमें नए अर्थों की खोज करता है ।
संरचना और संरचनावाद भाषिक दृष्टि से साहित्य के मूल्यांकन के प्रतिमान हैं। आधुनिक आलोचना में शैली वैज्ञानिक आलोचना भी ‘संरचनावाद’ पर विशेष बल देती है ।
‘संरचनावाद’ के अनुसार, हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त सम्पूर्ण संरचना के रूप में देखना चाहिए। यह सम्पूर्ण संरचना पर्त-दर-पर्त इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उपसंरचनाओं – ध्वनि, छंद, बिम्ब, पदविन्यास आदि के जाल के रूप में देखा जा सकता है ।
किसी रचना के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर साहित्य रचना के मूल सिद्धांतों का अन्वेषण ‘संरचनावाद’ का लक्ष्य है । संरचनावाद वस्तुत: समीक्षा को विज्ञान के निकट या समकक्ष रखने वाला आंदोलन है ।
संरचनावाद में विशेष बल विषयवस्तु (Content) पर न रहकर, उसकी रूपरचना या संरचना (Structure) पर दिया जाता है । इसमें किसी भी कृति के अर्थविधान और शब्दविधान (semantics and vocabulary) को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।
इसमें भाषा के अध्ययन में शैली विज्ञान को विशेष उपयोगी समझा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि संरचनावाद में मुख्य बल किसी कृति के ‘विषय पक्ष’ (subject matter) पर न देकर उसके ‘कलापक्ष’ (art) पर दिया जाता है ।
संरचनावाद में कविता या किसी भी कृति के शब्द विधान (wording/Vocabulary), भंगिमा Gesture), प्रतीक Symbol), संदिग्धता Ambiguity) आदि शिल्पगत तत्वों पर बारीकी से विचार किया जाता है । इसके अंतर्गत काव्यभाषा (poetic language) पर गंभीर चिंतन किया जाता है और उसके साथ ही काव्य में परंपरा और उसकी अखंडता (tradition and integrity) को महत्व प्रदान किया जाता है ।
संरचनावाद के मूल तत्व (Fundamentals of Structuralism)
नयी समीक्षा (New Criticism) के अंतर्गत ‘संरचनावाद’ एक नयी समीक्षा पद्धति है, जिसके अंतर्गत किसी रचना का संरचनावादी सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है ।
नयी समीक्षा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यह है कि समीक्षा का विषय साहित्यकार न होकर उसकी कृति ही होनी चाहिए। इसका कारण यह था कि मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद के प्रभाव में आकर साहित्य समीक्षा की प्रवृत्ति भी कृति की अपेक्षा कृतिकार के विश्लेषण में अधिक रस लेने लगी थी। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इस नयी समीक्षा का विकास हुआ।
जब हम किसी कृति पर विचार करते हैं, तब सबसे पहले हमारे सामने उसकी भाषायी संरचना (linguistic structure) आती है और यही भाषिक संरचना, संरचनावाद का प्रमुख विचार-बिन्दु है ।
शब्दावली, शब्दों की बनावट (Style) और बुनावट (Texture), शब्दों की पच्चीकारी (mosaic of words), अर्थ का ढांचा (Structure of meaning), शब्दार्थगत श्लेष (अनेकार्थता-semantic puns), संदेह (Ambiguity), विरोधाभास (contradiction), सादृश्य विधान (analogy), भावावेश (Internal Tension), आद्यंत गति और अर्थ-निर्वाह (External Tension) आदि अनेक प्रकार की सजावट या अलंकृति आदि नयी समीक्षा के अंतर्गत ‘संरचनावाद’ में विचार्य होती है ।
‘sanrachanavad’ में शब्द-विधान के साथ-साथ प्रतीक-विधान, लय-शब्द, भंगिमा, विरोधाभास, तनाव आदि को लेकर अलग-अलग समीक्षकों ने विचार किया है । ‘संरचनावाद’ में शब्द-विधान और अर्थ-विधान की समन्विति या बुनावट है। शब्द-विधान प्रधान होता है और वही मुख्य काव्य सौन्दर्य संपादित करता है ।
भंगिमा (Gesture) के अंतर्गत शब्द रचना, लय, छंद, अलंकार आदि सभी कुछ आ जाते हैं ।
‘संरचनावाद’ में मूल दृष्टिकोण यही है कि कृति में यह देखा जाए कि वस्तु (Content), भाव (Expression) और विचारपक्ष (Ideology) किस प्रकार संरचना अर्थात् शब्द, लय, अलंकृति (ornamentation) या कथन की भंगिमा (Utterance) में मिलकर एक रूप हो गया है और दोनों पक्ष मिलकर उस रचना को क्या आभा, क्या कान्ति और क्या सौन्दर्य प्रदान करते हैं ।
संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्त्रोत (Basic Source of the Concept of Structuralism)
‘sanrachanavad’ की अवधारणा का मूल स्त्रोत भाषा विज्ञान के प्रोफेसर सस्यूर (1857-1913) द्वारा प्रतिपादित भाषा सिद्धान्त है । सस्यूर के अनुसार भाषा के दो रूप हैं _(1) प्रथम ‘ल लांग’ तथा (2) दूसरा ‘ल परोल’। ‘ल लांग’ को अन्तर्वैयक्तिक (पारस्परिक) भाषा-व्यवस्था (interpersonal language system) कह सकते हैं। ‘ल परोल’ को व्यक्तिविशेष की भाषा (individual’s language) कहा जा सकता है ।
‘ल लांग’ अन्तः संबंधित प्रतीकों की ऐसी सामान्य व्यवस्था है, जो पूरे समाज में वैचारिक सम्प्रेषण संभव बनाती है । यह व्यवस्था भाषा-समूह के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है ।
‘ल परोल’ का क्षेत्र सीमित है । व्यक्ति-भेद से उसका रूप बदल जाता है । (उदाहरण- छौ-बिहार, छै-छत्तीसगढ़, छ: या छह- मानक हिंदी)। ‘अजय’ का परोल ‘अमित’ से भिन्न होगा। परोल स्वच्छन्द भी है और परिवर्तनशील भी है । उसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है । ‘लांग’ के नियमों से से ही ‘परोल’ नियंत्रित होता रहता है । ‘परोल’ (व्यक्तिभाषा) के रूप में ही लांग खंडश: मूर्त होता है ।
परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान ही ‘संरचना’ है । प्रसिद्ध नृतत्वशास्त्री लेवी स्त्रॉस ने इसी सिद्धान्त को मिथकों या पुराख्यानों के अध्ययन पर लागू किया । उसके अनुसार मूल मिथक ‘लांग’ है तो उसके अलग-अलग रूप ‘परोल’। मिथक के अलग-अलग रूपों के सिद्धान्त को रोलावार्थ ने प्रश्रय दिया ।
दूसरे शब्दों में भाषा संकेतों की एक प्रणाली है, इसकी अपनी एक संरचना होती है । ‘भाषा संकेतों की एक प्रणाली है’ – इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक संकेत के दो पक्ष या दो भाग होते हैं, पहला संकेतक (Signifier) और दूसरा संकेतित (Signified) । इन दोनों (संकेतक और संकेतित) से मिलकर किसी चिह्न या प्रतीक की रचना होती है ।
तात्पर्य यह है कि संकेतक का अर्थ संकेत देनेवाली किसी भौतिक वस्तु से है जो संकेत देकर हमारे व्यवहार को प्रभावित एवं परिचालित करती है । जैसे
चौराहे पर लगी हरी लाल बत्तियां । लाल बत्ती के जलने से हम रुक जाते हैं और हरी बत्ती के जलने पर हम चलने लगते हैं। संकेतित से तात्पर्य उस अर्थ से है जो अर्थ संकेतक को समाज देता है । उपर्युक्त उदाहरण में लाल रंग को खतरे के अर्थ में परिभाषित किया गया है । यह अर्थ समाज द्वारा दिया गया है ।
संरचनावाद के अनुसार हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त सम्पूर्ण संरचना के रूप में देखना चाहिए। यह सम्पूर्ण संरचना पर्त-दर-पर्त
इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उप-संरचनाओं – ध्वनि, छन्द, बिम्ब, पदविन्यास आदि के जाल के रूप में देखा जा सकता है ।
कृति विशेष की जटिल संरचना के विश्लेषण से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर अंततः साहित्य मात्र की रचना के मूल सिद्धान्तों का अन्वेषण ‘संरचनावाद’ का लक्ष्य है ।
अतः संरचनावाद केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना (lexical or linguistic structure) है जिसका झुकाव ‘रूपवाद’ की ओर अधिक है ।
संरचनावादी मूल्यांकन प्रविधि (Structuralist evaluation method)
संरचना और ‘sanrachanavad’ भाषिक दृष्टि से साहित्य के मूल्यांकन के प्रतिमान हैं । आधुनिक आलोचना में शैली वैज्ञानिक आलोचना भी संरचना पर विशेष बल देती है ।
संरचना (Structure) एक सावयव या संगतिनिष्ठ साकल्य (Organic Whole) के रूप में होती है । जैसे कि हमारा शरीर है जो विभिन्न अंगों (Organs)
से मिलकर बना है । ऐसी ही संरचना किसी वस्तु, व्यवस्था अथवा साहित्यिक कृति की हो सकती है । ‘संरचना’ विभिन्न भाषिक तत्वों जैसे कि ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ के बीच अन्वय संबंधों (Unity) पर निर्भर करती है ।
संरचना की इसी प्रकृति के कारण संरचना स्वयं में प्रेक्षणीय (दृष्टिगोचर) नहीं होती, किन्तु उसका परिज्ञान प्रेक्षण क्रिया द्वारा ही किया जाता है, जो दो प्रकार की होती है: 1) भाववादी (Sentimentalist) (2) वस्तुवादी (Objectivist)
भाववादी समीक्षक (प्रेक्षक) किसी कृति की अभ्यंतर प्रकृति (internal nature) को स्वयं समझना चाहता है और उसकी व्याख्या स्वयं की गई आत्मगत व्याख्या (subjective interpretation) होती है अर्थात् वह कृति में अंतर्निहित भाव की व्याख्या करता है, जबकि वस्तुवादी समीक्षक संरचना का केंद्र व्यक्ति को न मानकर वस्तु (कृति) को मानता है।
इस प्रकार संरचना प्रछन्न रूप से कृति की आंगिकता में निहित रहती है । (It means the structure implicitly lies in the originality of the work.)
संरचनावादी समीक्षक, शैली वैज्ञानिक अर्थात् वस्तुवादी अवधारणा (objective concept) के पक्षधर हैं, अर्थात् भाषायी दृष्टिकोण से कृति की समीक्षा करते हैं । अतः संरचनावाद में केन्द्रवर्ती बिन्दु ‘कृति’ ही ठहरती है, कृतिकार अथवा समीक्षक नहीं ।
संरचना की अवधारणा के आधारभूत तत्व (Fundamentals of the Concept of Structure
संरचना की अवधारणा तीन आधारभूत तत्वों पर निर्भर है – (1) अखंडता (Wholeness), (2) प्रयोजन (Purpose) और (3) स्वायत्तता (Autonomy) ।
अखंडता (Wholeness)
अखंडता का संबंध आंतरिक संगति (internal consistency) से है। किसी भी कृति के विभिन्न संघटक अंगों में एक विशेष अन्विति (Unity) होती है। कृति के संघटक तत्वों जैसे- शब्द, पद, पदबंध, वाक्य संरचना, वाक्य विन्यास में परिवर्तन करने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए- रंगीन पोशाक और रंगीन मिजाज में शब्द संसर्ग के कारण रंगीन का अर्थ अलग-अलग है ।
प्रयोजन (Purpose)
संरचना अपनी अर्थवत्ता से जुड़ी है । कवि विशेष प्रयोजन से ‘शब्द’ का प्रयोग अलग-अलग प्रकार से करता है । अर्थात शब्द का अर्थ उसके प्रयोजन पर निर्भर करता है । उदाहरण –
(i) कपड़े सीना, (ii) घाव सीना
(i) दवा पीना, (ii) खून पीना
(i) साबुन से हाथ धोना, (ii) जान से हाथ धोना
यहाँ प्रथम प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रयुक्त है, किंतु द्वितीय प्रयोग विडंबनापूर्ण दुखात्मक एवं हिंसक प्रवृत्तियों को रूपायित करने के लिए किए गए हैं।
स्वायत्तता (Autonomy)
अपनी सत्ता के लिए संरचना किसी अन्य पर आश्रित नहीं होती। संरचना के संघटक तत्वों के घात-प्रतिघात (संघर्ष) से ही उसका अर्थ व्यक्त होता है ।
संरचनावाद की मूल मान्यताएं (Basic Beliefs of Structuralism)
1. संरचनावाद का मूल आधार है- भाषिक दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन ।
2. संरचनावाद का संबंध प्रसिद्ध भाषाविद् सस्यूर के भाषा संबंधी अध्ययन से है ।
3. संरचनावाद का संबंध भाषा से है। जॉन लॉक की मान्यता है कि भाषा का स्वरूप बड़ा जटिल है। शब्द का सामान्य अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है और विशिष्ट अर्थ में भी। सस्यूर भाषा के दो तत्वों का उल्लेख करता है- (i) परोल (Parole) अर्थात् भाषा का भौतिक पक्ष तथा (ii) लेंगुई (Langue) जो भाषा का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ‘लेंगुई’ और ‘परोल’ (अर्थात भाषा और वाक्) की प्रक्रिया संरचना और संरचनावाद की जड़ में है। संरचना का परिवर्तन शब्दार्थ के परिवर्तन को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए कबीर और बिहारी के दो दोहे प्रस्तुत हैं :
(i) माली आवत देखि कै कलियन करी पुकार।
फूली-फूली चुनि लई काल्ह हमारी बार।।
– कबीर
(ii) नहिं पराग नहिं मधुर नहिं, नहिं विकास इहि काल।
अली कली ही सों विंध्यौ, आगे कौन हवाल॥ – बिहारी
उक्त दोनों दोहों में ‘कली’ शब्द का प्रयोग अलग-अलग अर्थ में हुआ है। कबीर ने कली (कलियन) का प्रयोग ‘नश्वर जीव’ की नश्वरता को व्यक्त करने के लिए किया है, तो बिहारी ने ‘कली’ का प्रयोग ‘अल्पायु में विवाहित किशोरी’ के लिए किया है । वस्तुतः यह अर्थ भेद प्रयोजन भेद के कारण है ।
4. संरचनावाद का सार तत्व ‘रूपवाद’ में निहित है। भाषा के अनेक घटक या अवयव हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं । ‘संरचनावाद’ किसी वस्तु, कृति, घटना और समाज का अध्ययन इसी सावयवी पद्धति (organic method) से करता है ।
5. संरचना अपने में पूर्ण होती है, चाहे वह साहित्यिक कृति की हो या मिथक की हो । वस्तुतः संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद को समझने के लिए ‘रूपवाद’ अथवा ‘रूसी रूपवाद’ को समझना आवश्यक है। रूपवाद साहित्यालोचन की ‘रूपनिष्ठ’ अर्थात् ‘काव्य भाषानिष्ठ’ समीक्षा है।
डॉ. नामवर सिंह की समीक्षाकृति ‘कविता के नए प्रतिमान’ पर ‘रूसी रूपवाद’ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।
6. रूपवादियों ने कृति को प्रथम स्थान दिया। वे कृति के सौन्दर्य और संदेश को कृति के भीतर खोजते हैं बाहर नहीं।
7. सस्यूर ने भाषा को एक व्यवस्था (System) माना है जिसका निर्माण चिन्हों (Symbols) सिंबल से हुआ है। एक भाषाई चिन्ह के दो तत्व होते हैं – स्वर बिम्ब और विचार। पहला तत्व ‘व्यंजक’ (Signifier) है और दूसरा तत्व ‘व्यंग्य’ (Signified) है। ‘हाथी’ कहने से हमारे मन में तुरंत हाथी का बिम्ब उभरता है । ये चिन्ह हमें हजारों वर्ष की भाषा परंपरा से प्राप्त हैं सस्यूर का विचार है कि भाषागत ये चिन्ह मनमाने ढंग से (Arbitrary) निर्मित हुए हैं और अलग-अलग समुदाय में अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग चिन्ह बने । भाषा विज्ञान और संरचनावाद को सस्यूर का यह अप्रतिम योगदान है।
शब्दगत संरचना नाना प्रकार के अनुभव जगत को रूपायित करती है, जिसे ‘संरचना’ का अध्ययन करके समझा जा सकता।
8. प्राग स्कूल के प्रमुख मुकारोवस्की ने साहित्य की प्रचलित समीक्षा पद्धति से भिन्न एक नई समीक्षा पद्धति पर बल दिया, जो ‘संरचना’ (Structure) और प्रकार्य (Function) पर बल देती है । वे कविता को भाषागत संरचना मानते हैं । उनकी दृष्टि में संरचना भाषाई तत्वों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है।
9. प्राग स्कूल के संरचनावाद के उपरांत सातवें-आठवें दशक दशक में फ्रांसीसी संरचनावाद का नया मॉडल सामने आया, जिसमें साकल्यवाद (Totality) दृष्टि विकसित हुई । रूपवादी हर ‘पाठ’ को ‘एक चिन्ह व्यवस्था, के रूप में देखते थे, जबकि फ्रांसीसी मॉडल साकल्यता (Totality) पर बल देता है । संरचनावादी साहित्य को भाषा का पर्याय मानते हैं, किंतु नई समीक्षा ने भाषिक विश्लेषण को महत्व देते हुए भी भाषा को साहित्य का पर्याय स्वीकार नहीं किया ।
10. आधुनिक संरचनावादियों में नृतत्व विज्ञानी क्लाड स्ट्रास और रोलां बार्थ प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त फूको, अल्थूसर लाकॉ आदि ने संरचनावाद पर गहराई से विचार किया। रोलांबार्थ ने ‘संस्कृति’ को भी भाषा माना और संस्कृतिधर्मी साहित्य (cultural literature) की व्याख्याएं प्रस्तुत कीं । आधुनिक संस्कृति की संरचना भी भाषा की तरह है। संरचनावाद पर लिखी उनकी कृति का नाम है – दि फैशन सिस्टम (The Fashion System)। उनके अनुसार, “अर्थ लेखक के पास न होकर पाठ की संरचना में निहित होता है।” साहित्य निर्माण में पांच तत्व काम करते हैं :
शब्द, पद, वाक्य, मुहावरा और सांस्कृतिकता । इनकी सही पकड़ ही संरचनावाद है।
11. समग्र रूप से कह सकते हैं कि संरचनावाद लेखकीय अनुभव और आलोचकीय ज्ञान को अकारथ और गौड़ मानते हुए पाठ निर्माण एवं पाठ
संरचना में छिपे तत्वों को उजागर करने पर अधिक बल देता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
‘sanrachanavad’ के लिए रचना केवल ‘शाब्दिक या भाषिक संरचना’ है । इसलिए रचनाकार के वैचारिक-भावात्मक अभिप्राय विवेचन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं आता। ऐसी दशा में, सब मिलाकर संरचनावाद का झुकाव रूपवाद की ओर होना स्वाभाविक है ।
इस तरह कुल मिलाकर संरचनावाद एक ऐसा वाद है जो लेखकीय अथवा आलोचकीय अनुभव को अकारथ और गौण मानता है और पाठ-निर्माण, पाठ-संरचना में छिपे तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करता है । इसका सार तत्व यह है कि पाठ की वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है और पैटर्न, व्यवस्था और संरचना पर नज़र टिक जाती है। इस प्रक्रिया में ‘लेखक’ का लोप हो जाता है । उसे दरकिनार करके ही चर्चा की जाती है ।
इस तरह हम कह सकते हैं कि संरचनावाद समकालीन साहित्य चिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन यह शुद्ध साहित्यिक सिद्धांत नहीं है । यह व्यापक सिद्धांत है जो अन्य अनुशासनों के साथ-साथ साहित्य पर भी लागू हो सकता है । सबसे पहले संरचनावाद का प्रयोग भाषा-विज्ञान में हुआ और भाषा-विज्ञान के रास्ते से यह साहित्य में आया। । ज्ञातव्य है कि यह भारतीय साहित्य चिंतन का हिस्सा नहीं है बल्कि भारत में यह यूरोपीय और विशेष रूप से फ्रेंच साहित्य से आया है । आलोचकों और विचारकों ने साहित्य की संरचनावादी व्याख्या की है । इससे साहित्य को नए ढंग से पढ़ने-समझने की दृष्टि मिली है ।
साहित्येतिहास के लिए कृति और कृतिकार की ऐतिहासिक चेतना और कलाचेतना के स्वरूप और संयोग प्रक्रिया का विश्लेषण आवश्यक है; जिसके लिए संरचनावादी साहित्य चिंतन में जगह नहीं है ।
‘sanrachanavad’ हिंदी में चर्चा-मात्र का ही विषय रहा है । अभी तक कोई ऐसी आलोचनात्मक कृति नहीं आयी है, जिसमें किसी रचना का अध्ययन-विश्लेषण संरचनावाद के आधार पर किया गया हो ।

नमस्कार ! मेरा नाम भूपेन्द्र पाण्डेय है । मेरी यह वेबसाइट शिक्षा जगत के लिए समर्पित है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और अनुवाद विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य है । मैं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ।
मेरे लेक्चर्स हिंदी के छात्रों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं ।
मेरी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है : बीएससी, एमए (अंग्रेजी) , एमए (हिंदी) , एमफिल (हिंदी), बीएड, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन (गोल्ड मेडल), यूजीसी नेट (हिंदी), सेट (हिंदी)
मेरे यूट्यूब चैनल्स के नाम : Bhoopendra Pandey Hindi Channel, Hindi Channel UPSC