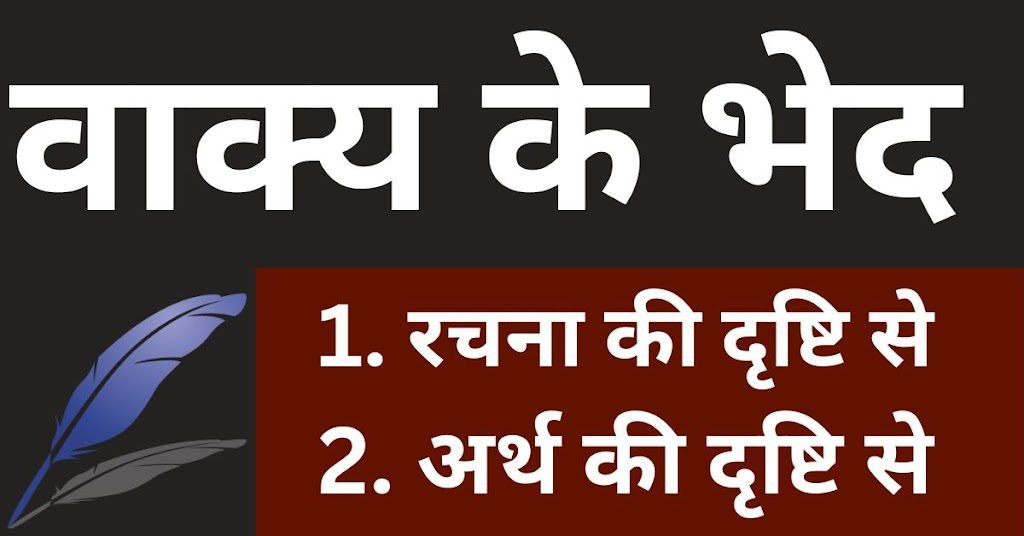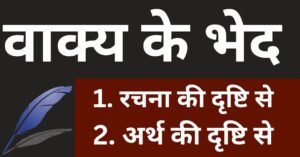शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग-अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। जबकि शब्दों को निश्चित क्रम और स्वाभाविक गति से बोलने पर वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।
जैसे – नदी के किनारे-किनारे एक गाय जा रही थी।
अतः हम कह सकते हैं-
वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता अथवा सामर्थ्य होता है।
वाक्य के अंग (Parts of Sentence)
वाक्य के दो अंग होते हैं- (1) उद्देश्य (Subject) (2) विधेय (Predicate)
एक छोटा-सा वाक्य लें – राहुल आया।
इसके दो अंग हैं- 1. राहुल 2. आया।
यहाँ राहुल के बारे में बात की गई है अतः ‘राहुल’ वाक्य का उद्देश्य(Subject) है। राहुल के बारे में कहा गया है कि वह ‘आया’। यहाँ ‘आया’ विधेय (Predicate) है।
उद्देश्य (Subject)
वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य (Subject) कहते हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को ‘उद्देश्य का विस्तार’ कहा जाता है। जैसे – झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया।
लक्ष्मीबाई – उद्देश्य है और ‘झाँसी की रानी’ उद्देश्य का विस्तार है।
विधेय (Predicate)
उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वह विधेय (Predicate) होता है। विधेय का भी विस्तार हो सकता है।
जैसे- मैंने बड़ी रुचि से पुस्तक पढ़ी।
पुस्तक पढ़ी – विधेय
बड़ी रुचि से – विधेय का विस्तार
कुछ अन्य उदाहरण देखिए :
| उद्देश्य (Subject) | विधेय (Predicate) |
| भागता हुआ चोर | तुंरत पकड़ा गया। |
| वह बेचारा | क्या कर सकता था। |
| सुंदर मोर |
पंख फैलाकर नाच रहा है।
|
उपर्युक्त वाक्यों में भागता हुआ, बेचारा, सुंदर – उद्देश्य के विस्तार हैं।
तुरंत, क्या, पंख फैलाकर – विधेय के विस्तार हैं।
नोट :
1. कभी-कभी उद्देश्य (Subject) प्रकट नहीं होता। जैसे- ‘आओ’ एक वाक्य है। इसमें तुम (उद्देश्य) अप्रकट है, पूरा वाक्य होगा- ‘तुम आओ।’
2. कभी-कभी विधेय (Predicate) भी लुप्त रहता है। जैसे – कोई पूछता है- कौन आएगा? उत्तर है – ‘मैं’। पूरा वाक्य होगा- मैं आऊँगा। यहाँ ‘आऊँगा’ विधेय अप्रकट है।
वाक्य के भेद (Kinds of Sentence) Vakya ke Bhed
वाक्य को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है-
1. रचना की दृष्टि से
2. अर्थ की दृष्टि से
रचना की दृष्टि से वाक्य भेद (Rachna ki Dridhti se Vakya ke Bhed)
रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं :
(क) सरल वाक्य
(ख) संयुक्त वाक्य
(ग) मिश्र वाक्य
(क) सरल वाक्य (Simple Sentence)
जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य (Simple Sentence) कहते हैं। सरल वाक्य में उद्देश्य (Subject) तो एक से अधिक हो सकते हैं, पर विधेय (Predicate) एक ही होता है।
उदाहरण-
1. विकास आया।
2. अजय ने खाना खाया।
3. एक लड़का और चपरासी पहुँच गए।
4. रागिनी, राहुल और सलीम आ गए हैं।
ऊपर के पहले दो वाक्यों में उद्देश्य (Subject) में एक-एक पद है, तीसरे वाक्य में दो और चौथे वाक्य तीन।
परंतु चारों वाक्यों में विधेय (Predicate) एक-एक ही है। ये सब सरल वाक्य हैं। सरल वाक्यों में एक विधेय (Predicate) होता है।
(ख) संयुक्त वाक्य (Compound Sentence)
इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य (Simple Sentence) योजक के द्वारा जुड़े होते हैं।
उदाहरण-
1. राहुल स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है।
2. वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया।
3. आप ठंडा लेंगे अथवा चाय मँगवाऊँ?
(ग) मिश्र वाक्य (Complex Sentence)
जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वह मिश्र वाक्य कहलाता है।
मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य (Simple Sentence) होते हैं; परंतु इनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित उपवाक्य होता है ।
उप वाक्य (Clause)
ऐसा पद समूह, जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है।
उदाहरण – राजीव ने कहा कि मैं खेलूँगा ।
इसमें ‘राजीव ने कहा’ प्रधान उपवाक्य है और ‘कि मैं खेलूँगा’ आश्रित उपवाक्य।
उपवाक्य के प्रकार
उप वाक्य तीन प्रकार के होते हैं –
(1) संज्ञा-उपवाक्य (Noun Clause), (2) विशेषण-उपवाक्य (Adjective Clause), (3) क्रियाविशेषण-उपवाक्य (Adverb Clause)
संज्ञा-उपवाक्य (Noun Clause)
जिस उपवाक्य का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है, उसे संज्ञा-उपवाक्य कहते हैं ।
उदाहरण : अजय ने कहा कि मैं पढ़ूँगा ।
यहाँ ‘मैं पढ़ूँगा’ संज्ञा-उपवाक्य है ।
विशेषण-उपवाक्य (Adjective Clause)
जिस उपवाक्य का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है, उसे
विशेषण-उपवाक्य कहते हैं ।
उदाहरण : वह आदमी, जो कल आया था, आज भी आया है।
यहाँ ‘जो कल आया था’ विशेषण-उपवाक्य है ।
इसमें प्रायः ‘जो’, ‘जैसा’, ‘जितना’ इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है ।
क्रियाविशेषण-उपवाक्य (Adverb Clause)
जिस उपवाक्य का प्रयोग क्रियाविशेषण की तरह किया जाता है, उसे क्रियाविशेषण-उपवाक्य कहते हैं ।
उदाहरण : जब पानी बरसता है, तब मेढक टर्राते हैं । ।
यहाँ ‘जब पानी बरसता है’ क्रियाविशेषण-उपवाक्य है ।
इसमें ‘जब’, ‘जहाँ’, ‘जिधर’, ‘ज्यों’, ‘यद्यपि’ इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है ।
नोट – उपवाक्यों के आरंभ में प्रायः कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों-ज्यों, चूँकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि होते हैं ।
कृपया इसे भी पढ़ें : समास और उसके प्रकार
मिश्र वाक्य के उदाहरण-
1. राहुल ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे?
‘राहुल ने पूछा’ – प्रधान उपवाक्य
कि तुम कहाँ गए थे – आश्रित उपवाक्य
2. हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएँगे, जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है।
‘हम जानते हैं’ – प्रधान उपवाक्य
कि वे आज नहीं आएँगे – आश्रित उपवाक्य
उनकी अत्यंत आवश्यकता है। – आश्रित उपवाक्य
अन्य उदाहरण-
1. वह बालक खड़ा हो जाए, जिसने शीशा तोड़ा है।
वह बालक खड़ा हो जाए – प्रधान उपवाक्य
जिसने शीशा तोड़ा है – आश्रित उपवाक्य
2. जहाँ-जहाँ हम गए, हमारा भव्य स्वागत हुआ। हमारा भव्य स्वागत हुआ
हमारा भव्य स्वागत हुआ – प्रधान उपवाक्य
जहाँ-जहाँ हम गए – आश्रित उपवाक्य
वाक्य परिवर्तन
1.लाल बत्ती होते ही यातायात रुक गया। (सरल वाक्य)
लाल बत्ती हुई और यातायात रुक गया। (संयुक्त वाक्य)
जैसे ही लाल बत्ती हुई, यायायात रुक गया। (मिश्र वाक्य)
2. घंटी बजी। छात्र घर चले गए। (दो सरल वाक्य)
घंटी बजते ही छात्र घर चले गए। (एक सरल वाक्य)
जब घंटी बजी, छात्र घर चले गए। (मिश्र वाक्य)
3. रवि को संस्कृत पढ़नी है और वह शिक्षक के घर गया है। (संयुक्त वाक्य)
रवि संस्कृत पढ़ने के लिए शिक्षक के घर गया है। (सरल वाक्य)
रवि शिक्षक के घर गया है क्योंकि उसे संस्कृत पढ़नी है। (मिश्र वाक्य)
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद (Arth ki Drishti se Vakya ke Bhed)
अर्थ की दृष्टि से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं-
1. विधानार्थक वाक्य (Assertive Sentence)
2. निषेधार्थक वाक्य (Negative Sentence)
3. प्रश्नार्थक वाक्य (Interrogative Sentence)
4. आज्ञार्थक वाक्य (Imperative Sentence)
5. संदेहार्थक वाक्य (Presumptive Sentence)
6. संकेतार्थक वाक्य (Conditional Sentence)
7. इच्छार्थक वाक्य (Optative Sentence)
8. विस्मयार्थक वाक्य (Exclamatory Sentence)
अब हम इनका विस्तार से अध्ययन
करेंगे ।
विधानार्थक वाक्य (Assertive Sentence)
इस प्रकार के वाक्य में किसी बात या काम के होने का सामान्य बोध होता है।
जैसे- वह आया।
ठंडी हवा चल रही है।
निषेधार्थक वाक्य (Negative Sentence)
इस प्रकार के वाक्यों में किसी काम के निषेध अर्थात् न करने या न होने का भाव रहता है।
जैसे- वह नहीं आएगा।
मैं कुछ नहीं कर सकूँगा।
प्रश्नार्थक वाक्य (Interrogative Sentence)
इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है।
जैसे- तुम क्या कर रहे हो?
वह कब आया?
आज्ञार्थक वाक्य (Imperative Sentence)
इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा दी जाती है अथवा अनुरोध किया जाता है।
जैसे- तुम यहाँ से चले जाओ।
किसी का दिल मत दुखाओ।
संदेहार्थक वाक्य (Presumptive Sentence)
इस प्रकार के वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है।
जैसे- शायद आज वर्षा हो।
हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े।
संकेतार्थक वाक्य (Conditional Sentence)
इस प्रकार के वाक्य में एक बात या कार्य का होना, किसी दूसरी बात या कार्य पर निर्भर रहता है। इसमें शर्त होती है।
जैसे- यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी।
यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते।
इच्छार्थक वाक्य (Optative Sentence)
इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना या अभिशाप का भाव प्रकट किया जाता है।
जैसे- तुम्हारा कल्याण हो।
आपकी यात्रा शुभ हो।
विस्मयार्थक वाक्य (Exclamatory Sentence)
इन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं।
जैसे- अरे! तुम भी आ गए।
वाह! तुमने कमाल कर दिया।
हाय! यह क्या हो गया?
वाक्य-परिवर्तन
1. मैं पत्र लिख रहा हूँ।
मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। (निषेधार्थक वाक्य में)
2. वह पाठ पढ़ेगा।
क्या वह पाठ पढ़ेगा? (प्रश्नार्थक वाक्य में)
3. तुम यहाँ से चले जाओ।
अरे! तुम यहाँ से चले जाओगे। (विस्मयार्थक वाक्य में)
4. राहुल आज जाएगा।
राहुल आज शायद ही जाए। (संदेहार्थक वाक्य में)
निष्कर्ष
Vakya ke Bhed | Vakya ke Prakar
1. सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनता है।
2. वाक्य के दो अंग होते हैं- उद्देश्य और विधेय।
3. रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं- सरल, संयुक्त, मिश्र।
4. अर्थ की दृष्टि से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं- विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञा संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक और विस्मयार्थक।

नमस्कार ! मेरा नाम भूपेन्द्र पाण्डेय है । मेरी यह वेबसाइट शिक्षा जगत के लिए समर्पित है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और अनुवाद विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य है । मैं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ।
मेरे लेक्चर्स हिंदी के छात्रों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं ।
मेरी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है : बीएससी, एमए (अंग्रेजी) , एमए (हिंदी) , एमफिल (हिंदी), बीएड, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन (गोल्ड मेडल), यूजीसी नेट (हिंदी), सेट (हिंदी)
मेरे यूट्यूब चैनल्स के नाम : Bhoopendra Pandey Hindi Channel, Hindi Channel UPSC